काका कालेलकर: भारत के आत्मा-स्पर्शी समाज सुधारक और गांधीवादी शिक्षाविद(22 अप्रैल 1885- 21 अगस्त 1981)
प्रारंभिक जीवन और संस्कार
धनंजय कीर्ति कालेलकर, जिन्हें प्रेम से ‘काका’ कहा जाता था, का जन्म 22 अप्रैल 1885 को महाराष्ट्र के सत्तारा ज़िले में हुआ था।
वे एक मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जहाँ परंपरागत भारतीय शिक्षा और संस्कृति का माहौल था।
बचपन से ही उनके भीतर एक चिंतनशील, सहृदय और सामाजिक प्रवृत्ति दिखाई देती थी।
उनकी शिक्षा पुणे और फिर गुजरात कॉलेज, अहमदाबाद में हुई। पढ़ाई के दौरान ही वे लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए।
यहाँ से उनका झुकाव राष्ट्र सेवा और सामाजिक न्याय की ओर हुआ।
गांधीजी के शिष्यत्व में जीवन परिवर्तन
1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो काका कालेलकर उन कुछ युवाओं में थे जो गांधीजी के विचारों से गहरे प्रभावित हुए।
वे साबरमती आश्रम से जुड़ गए और वहां उन्होंने ब्रह्मचर्य, स्वावलंबन, और साधारण जीवन को अपनाया।
उन्होंने स्वयं खादी पहनी, चरखा चलाया और अस्पृश्यता उन्मूलन को जीवन का ध्येय बनाया।
गांधीजी ने जब गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, तो कालेलकर को प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया।
वहाँ उन्होंने स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास किया।
उन्होंने शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखते हुए, उसे चरित्र निर्माण और राष्ट्रीयता के प्रसार का माध्यम बनाया।
स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी
काका कालेलकर ने गांधीजी के नेतृत्व में कई आंदोलनों में भाग लिया:
असहयोग आंदोलन (1920)
नमक सत्याग्रह (1930)
व्यक्तिगत सत्याग्रह (1940)
इन आंदोलनों में भाग लेने के लिए उन्हें कई बार कारावास भी झेलना पड़ा।
उनकी विचारशीलता और संयम ने उन्हें एक आदर्श गांधीवादी कार्यकर्ता के रूप में स्थापित कर दिया।
सामाजिक सुधार और पिछड़ा वर्ग आयोग (Kalelkar Commission)
स्वतंत्रता के बाद, भारत में सामाजिक विषमता और जातीय असमानता की समस्याएं प्रमुख थीं।
1953 में भारत सरकार ने उन्हें पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस आयोग का उद्देश्य था:
सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना।
उनके उत्थान के लिए ठोस नीतियाँ और सुझाव देना।
1955 में प्रस्तुत रिपोर्ट में काका कालेलकर ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं:
शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण
पिछड़े वर्गों को अर्थिक सहायता और छात्रवृत्तियाँ
समाज में समानता, जागरूकता और जातीय समरसता को बढ़ावा देना
हालाँकि सरकार ने तत्काल इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, परन्तु यह रिपोर्ट मंडल आयोग और बाद की नीतियों की नींव बन गई।
काका कालेलकर ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखा:
"आरक्षण केवल सामाजिक न्याय का औजार नहीं, यह आत्म-संवेदना और समाज के पुनर्जागरण का माध्यम है।"
साहित्यिक योगदान
काका कालेलकर केवल समाजसेवी ही नहीं, एक मेधावी लेखक और चिंतक भी थे।
उन्होंने मराठी, हिंदी और गुजराती में अनेक पुस्तकें और लेख लिखे जिनमें भारतीय संस्कृति, समाज, शिक्षा और नैतिक मूल्यों पर गहरा विश्लेषण किया गया है।
प्रमुख रचनाएँ:
1. "Atma-Vrittanta" (आत्मकथा) – उनके जीवन की ईमानदार झलकियों से भरपूर।
2. "Rashtriya Shikshan" – राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा और आवश्यकताओं पर लेख।
3. "Jeevan-Vyavastha" – भारतीय समाज में जीवन की संरचना पर विचार।
4. "Bapu-Ki Karvat" – गांधीजी के साथ बिताए पलों का आत्मीय चित्रण।
5. "Bhagavad Gita" पर भाष्य – गीता के गांधीवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण।
उनकी लेखनी गूढ़ होते हुए भी सरल भाषा में होती थी, जिससे आम जनता भी उनसे जुड़ पाती थी।
आध्यात्मिक जीवन और दर्शन
काका कालेलकर का जीवन कर्मयोग और आत्मनिष्ठा का अद्भुत संगम था।
उन्होंने वेदों, उपनिषदों और भगवद्गीता का गहन अध्ययन किया।
वे मानते थे कि व्यक्तिगत आत्म-शुद्धि ही सामाजिक परिवर्तन की पहली शर्त है।
उनका जीवन “साधना और सेवा” की मिसाल था।
सम्मान और पुरस्कार
उनके सामाजिक, शैक्षिक और साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए:
पद्म विभूषण (1964) – भारत सरकार द्वारा
गांधी स्मृति पुरस्कार
कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियाँ प्रदान कीं।
अंतिम दिन और विरासत
21 अगस्त 1981 को काका कालेलकर का देहांत हुआ, परंतु उनकी सोच, विचारधारा और आदर्श आज भी जीवित हैं।
उनकी विरासत:
गांधीवादी चिंतन का सजीव उदाहरण
जातिवादी संरचना के विरुद्ध सामाजिक चेतना
शिक्षा और सेवा का अनुपम आदर्श
भारत की सामाजिक नीति निर्माण की नींव में उनका नाम अंकित है
काका कालेलकर का जीवन भारत की आत्मा से संवाद है।
उन्होंने न केवल एक विचारशील समाज की कल्पना की, बल्कि उसे अपने जीवन से मूर्त रूप देने का प्रयास









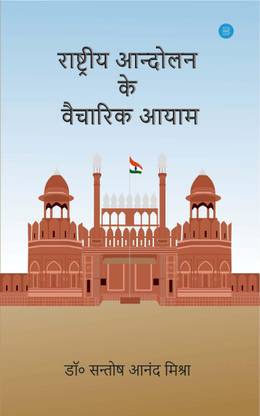



1 Comments
🙏🙏🙏🙏🙏
ReplyDeleteThank you