भूमिका
भारत के नवजागरण काल में अनेक महापुरुषों ने अपने विचारों, कर्मों और संघर्षों से समाज को नई दिशा दी। उनमें से एक प्रमुख नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का है, जिन्होंने अंधविश्वास, मूर्तिपूजा, जातिवाद और कुरीतियों से ग्रस्त समाज में सत्य, वेदज्ञान और राष्ट्रभक्ति की ज्योति प्रज्वलित की। वे भारतीय पुनर्जागरण के सच्चे प्रवर्तक और आर्य समाज के संस्थापक थे।
प्रारंभिक जीवन
स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ई. को गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र के टंकारा गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम अमृतलालजी तिवारी और माता का नाम यशोदा बाई था। उनका प्रारंभिक नाम मूलशंकर था। उनका परिवार अत्यंत धार्मिक था और बचपन से ही उनमें धार्मिक भावना और जिज्ञासा प्रबल थी।
आध्यात्मिक जागृति
मूलशंकर का जीवन एक साधारण धार्मिक बालक से एक महान संत तक का अद्भुत सफर रहा। महाशिवरात्रि की एक रात उन्होंने देखा कि मंदिर में रखे शिवलिंग पर चूहे दौड़ रहे हैं और फिर भी उसे ‘भगवान’ कहा जा रहा है। इस घटना ने उनके मन में मूर्तिपूजा के प्रति संदेह उत्पन्न किया। उन्होंने सत्य की खोज में घर त्याग दिया और अनेक वर्षों तक वनों, आश्रमों और गुरुकुलों में भ्रमण कर वेद, उपनिषद, दर्शन और संस्कृत व्याकरण का गहन अध्ययन किया।
आर्य समाज की स्थापना
सन् 1875 ई. में उन्होंने मुंबई (तत्कालीन बंबई) में आर्य समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था –
1. वेदों के प्रचार द्वारा सच्चे धर्म का प्रसार,
2. समाज से अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद का उन्मूलन,
3. स्त्रियों की शिक्षा और समान अधिकार का समर्थन,
4. धर्मांतरित भारतीयों का पुनर्वास (शुद्धि आंदोलन),
5. राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी भावना का विकास।
आर्य समाज ने भारत में सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रसार और राष्ट्रभक्ति की नई लहर पैदा की।
ग्रंथ और साहित्यिक योगदान
स्वामी दयानंद ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं –
1. सत्यार्थ प्रकाश – उनके विचारों और दर्शन का मुख्य ग्रंथ।
2. ऋग्वेद भाष्य और यजुर्वेद भाष्य – वेदों की व्याख्या।
3. संस्कृत व्याकरण पर अनेक ग्रंथ – जिनसे उन्होंने वेदभाषा को सुलभ बनाया।
‘सत्यार्थ प्रकाश’ में उन्होंने अंधविश्वासों की आलोचना और सत्य के मार्ग का प्रतिपादन किया।
वेदों की ओर लौटो: धर्म सुधार का मूल मंत्र
स्वामी दयानंद ने अपने गहन चिंतन और शास्त्रार्थों के बल पर यह सिद्ध किया कि तत्कालीन हिंदू धर्म का स्वरूप विकृत हो चुका है। उनका नारा "वेदों की ओर लौटो" (Go Back to the Vedas) मात्र एक धार्मिक आह्वान नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का संदेश था।
ईश्वर का स्वरूप: उन्होंने ईश्वर को सच्चिदानंद, निराकार, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ बताते हुए मूर्तिपूजा का खंडन किया। उनका मानना था कि ईश्वर की पूजा करने के लिए किसी मंदिर या मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शुद्ध हृदय और कर्म की आवश्यकता है।
तर्क और विज्ञान पर बल: उन्होंने वेदों को तर्क और विज्ञान-सम्मत बताया। अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कारों को खारिज करते हुए उन्होंने भारतीयों को तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया।
शुद्धि आंदोलन: उन्होंने धर्मांतरित भारतीयों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए 'शुद्धि आंदोलन' चलाया। यह उस समय की एक क्रांतिकारी पहल थी, जिसने हिंदू समाज को आत्मरक्षा और आत्मगौरव की भावना प्रदान की।
सामाजिक क्रांति के जनक
स्वामी दयानंद ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक बने।
जातिवाद का खंडन: उन्होंने जन्म आधारित जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया और कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। उनके अनुसार, हर व्यक्ति को अपने गुणों और कर्मों के आधार पर जाना जाना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर।
नारी सशक्तिकरण: वह महिला सशक्तिकरण के प्रखर पक्षधर थे।
उन्होंने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि वेदों के अध्ययन का अधिकार पुरुषों के समान स्त्रियों को भी है।
उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, और देवदासी प्रथा का कड़ा विरोध किया।
उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसके लिए सामाजिक माहौल बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित करने का सुझाव दिया।
अस्पृश्यता का उन्मूलन: उन्होंने छुआछूत (अस्पृश्यता) को सामाजिक कलंक बताया और इसके उन्मूलन के लिए प्रभावशाली उपाय किए।
राष्ट्रवाद और स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक
स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। उनके विचारों ने परतंत्रता की आत्मग्लानि से उबरने और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई।
स्वराज्य का नारा: उन्होंने सन् 1876 ई. में सबसे पहले 'स्वराज्य' (स्वशासन) की मांग उठाई। इस विचार को बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया।
स्वदेशी का विचार: उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं और मूल्यों को अपनाने पर बल दिया। उनका मानना था कि भारत का उत्थान भारतीयों द्वारा ही संभव है। उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का भी समर्थन किया, जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
वीर सपूतों की प्रेरणा: लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, और मदनमोहन मालवीय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी सीधे तौर पर उनके विचारों और आर्य समाज से प्रभावित थे, जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया।
शैक्षणिक विरासत: डीएवी और गुरुकुल
स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया, वह उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है।
दयानंद एंग्लो वैदिक (DAV) संस्थाएं: उनके अनुयायियों द्वारा स्थापित ये संस्थाएं वैदिक ज्ञान और आधुनिक (एंग्लो) शिक्षा का अद्भुत समन्वय हैं। इनका उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति की जड़ों से जोड़े रखते हुए आधुनिक विज्ञान और ज्ञान से लैस करना था।
गुरुकुल प्रणाली: स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की, जहाँ छात्रों को प्राचीन वैदिक शिक्षा और आधुनिक विषयों का ज्ञान दिया जाता था।
सत्यार्थ प्रकाश: एक कालजयी ग्रंथ
उनकी सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति 'सत्यार्थ प्रकाश' है, जिसे भारतीय पुनर्जागरण का घोषणापत्र कहा जा सकता है।
विषय वस्तु: यह ग्रंथ उनके विचारों, दर्शन, धार्मिक समालोचना, सामाजिक कुरीतियों का खंडन और वैदिक धर्म के सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करता है।
भाषा: उन्होंने इस ग्रंथ की रचना हिंदी भाषा में की, जिससे यह ग्रंथ जन-जन तक पहुँच सका और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में सहायक हुआ।
मृत्यु
स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन संघर्ष और सेवा से भरा था। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के आमंत्रण पर वे जोधपुर गए, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने उन्हें विष दे दिया। अंततः 30 अक्टूबर 1883 ई. को अजमेर में उन्होंने देह त्याग किया।
निष्कर्ष
स्वामी दयानंद सरस्वती सच्चे अर्थों में युग-निर्माता थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में तीन मोर्चों पर संघर्ष किया:
रूढ़िवादी हिंदू समाज से पाखंड और अंधविश्वासों के लिए।
ईसाई और मुस्लिम मतों से धर्म परिवर्तन के विरोध में।
ब्रिटिश सत्ता से स्वराज्य और राष्ट्रवाद के पक्ष में।
उनका योगदान भारतीय समाज को आत्मनिर्भर, तर्कशील, संगठित और आत्मगौरव से युक्त करने में अतुलनीय है। वे एक ऐसे महान नेता थे, जिन्होंने भारत को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया।













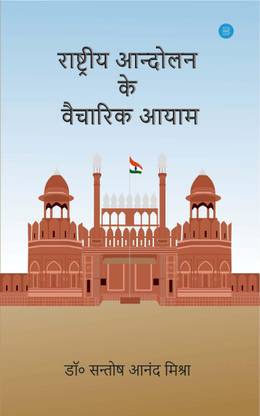





0 Comments
Thank you