मोहम्मद रफ़ी: स्वर का सम्राट, भावनाओं का बादशाह(24 दिसंबर 1924- 31 जुलाई 1980 )
भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास में कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो समय, भाषा और सीमाओं को लांघकर अमर हो जाते हैं। इन अमर स्वरों के शिखर पर प्रतिष्ठित हैं मोहम्मद रफ़ी। वे केवल एक पार्श्वगायक नहीं थे, बल्कि भारतीय जनमानस की भावनाओं का एक जीवंत माध्यम थे। उनकी आवाज़ में दर्द, प्रेम, भक्ति, उल्लास, देशभक्ति और हास्य का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण था, जो सीधे श्रोता के हृदय में उतर जाता था। आज भी, सुरों के मंदिर में मोहम्मद रफ़ी का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है।
प्रारंभिक जीवन: संगीत की पहली आहट
मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब (तत्कालीन ब्रिटिश भारत, अब पाकिस्तान में) के कोटला सुल्तान सिंह गाँव, जिला अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद और माता का नाम अल्लाह राखी बीबी था।
रफ़ी साहब का संगीत की ओर रुझान बचपन से ही स्पष्ट था। वे सड़कों पर फकीरों द्वारा गाए जाने वाले सूफियाना कलाम और मजारों पर होने वाली कब्बालियों से बहुत प्रभावित थे। उनकी इसी प्रतिभा को पहचानते हुए, उनके बड़े भाई हमीद ने उन्हें संगीत की औपचारिक शिक्षा दिलवाने के लिए लाहौर भेजा। लाहौर संगीत का एक बड़ा केंद्र था, जहाँ रफ़ी साहब को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद वहिद खां और पंडित जी.ए. चिश्ती जैसे महान गुरुओं के सानिध्य में रियाज़ करने का अवसर मिला। यहीं से एक युग-निर्माता गायक की नींव पड़ी।
संगीत करियर की शुरुआत: एक नया अध्याय
रफ़ी साहब ने अपने गायन करियर की शुरुआत 1941 में लाहौर से की, जहाँ उन्होंने एक पंजाबी फिल्म 'गुल बलोच' में अपना पहला गीत गाया। इसके बाद, सपनों के शहर मुंबई (तत्कालीन बंबई) ने उन्हें अपनी ओर खींचा और वे 1944 में वहाँ आ गए। हिंदी फिल्म जगत में उनका पहला कदम फिल्म 'पहेली नज़र' (1944) के गीत "हिन्दुस्तान के हम हैं" के साथ पड़ा, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया।
ब्रेकथ्रू और स्वर्णिम युग: सुरों का जादू
1940 के दशक के उत्तरार्ध और 1950 के दशक ने रफ़ी साहब के करियर में स्वर्णिम युग का सूत्रपात किया। उन्होंने उस दौर के दिग्गज संगीतकारों जैसे नौशाद, शंकर-जयकिशन, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन और ओ.पी. नैयर के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक अमर गीतों को जन्म दिया। उनकी आवाज़ हर संगीतकार की धुन में ऐसे घुल-मिल जाती थी, मानो वह उस धुन के लिए ही बनी हो।
उनके कुछ प्रमुख और कालजयी गीत:
"मन तड़पत हरि दर्शन को आज" | बैजू बावरा | 1952 |
"तेरी प्यारी प्यारी सूरत को" | साहिब बीबी और गुलाम |
1962 |
चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे" | दोस्ती | 1964 |
ए मेरी ज़ोहराजबीं" | वक्त | 1965 |
दिल तेरा दीवाना" | दिल तेरा दीवाना | 1962 |
"आज मौसम बड़ा बेईमान है" | लोफर | 1973 |
"क्या हुआ तेरा वादा" | हम किसी से कम नहीं | 1977 |
"बाहों में चले आओ" (कोरस में प्रमुख) | अनुरोध | 1977 |
स्वर की बहुआयामी विशेषताएँ: एक अद्वितीय प्रतिभा
मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को 'स्वर का सम्राट' यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी गायन शैली में कई ऐसी विशेषताएँ थीं, जो उन्हें अन्य गायकों से अलग बनाती थीं:
* भावनात्मक गहराई: उनकी आवाज़ में भावनाओं की अद्वितीय अभिव्यक्ति होती थी। चाहे वह दर्दभरा विरह गीत हो, चुलबुला रोमांटिक गीत हो, या गहन भक्ति गीत, रफ़ी साहब हर भावना को पूरी शिद्दत से अभिव्यक्त करते थे।
* अविश्वसनीय विविधता: रफ़ी साहब ने भक्ति गीतों, देशभक्ति गीतों, हास्य गीतों, ग़ज़लों, लोकगीतों और शास्त्रीय गीतों सहित हर शैली में महारत हासिल की। वे किसी भी शैली में खुद को ढाल लेते थे।
* विभिन्न अभिनेताओं की आवाज़: यह उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वे देव आनंद के लिए चुलबुली, दिलीप कुमार के लिए दर्द भरी, राजेंद्र कुमार के लिए रोमांटिक, शम्मी कपूर के लिए जोशीली, जॉनी वॉकर के लिए हास्यपूर्ण और राजेश खन्ना के लिए भावुक आवाज़ देने में सक्षम थे। वे हर अभिनेता के व्यक्तित्व में अपनी आवाज़ को ऐसे ढाल लेते थे कि लगता था अभिनेता खुद ही गा रहा है।
* मधुर और स्पष्ट उच्चारण: रफ़ी साहब का उच्चारण त्रुटिहीन था। उन्होंने हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तेलुगू, कन्नड़, गुजराती, सिंधी और यहां तक कि कुछ विदेशी भाषाओं में भी गीत गाए। हर भाषा और उसके उच्चारण पर उनकी कमाल की पकड़ थी।
प्रमुख संगीतकारों के साथ सहयोग: संगीतमय जुगलबंदी
रफ़ी साहब का करियर महान संगीतकारों के साथ उनकी सफल जुगलबंदियों से भरा पड़ा है। उन्होंने कई संगीतकारों के साथ मिलकर ऐसे गीत दिए जो आज भी सदाबहार हैं:
* नौशाद: "ओ दुनिया के रखवाले", "मन तड़पत हरि दर्शन को आज" जैसे भक्ति और शास्त्रीय प्रभाव वाले गीत।
* मदन मोहन: "तेरी आँखों के सिवा", "रंग और नूर की बारात", "तुझको पुकारे मेरा प्यार" जैसे ग़ज़ल और भावुक गीत।
* ओ.पी. नैयर: "ये है बॉम्बे मेरी जान", "मेरा नाम चिन चिन चू", "पुकारता चला हूँ मैं" जैसे वेस्टर्न और पेपी नंबर्स।
* लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल (एल.पी.): "क्या हुआ तेरा वादा", "दीवाना हुआ बादल", "छलकाए जाम" जैसे असंख्य हिट।
* आर.डी. बर्मन: "गुलाबी आंखें", "यम्मा यम्मा", "चुरा लिया है तुमने" (आशा भोसले के साथ) जैसे युवा और आधुनिक धुनें।
पुरस्कार और सम्मान: एक अपूर्ण सूची
रफ़ी साहब को अपने करियर में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:
* राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: 1977 में फिल्म 'हम किसी से कम नहीं' के गीत "क्या हुआ तेरा वादा" के लिए।
* फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार: उन्होंने 6 बार फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार जीता, जो उनकी लोकप्रियता और गुणवत्ता का प्रमाण है।
* पद्म श्री: 1967 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया।
यह आज भी एक अफसोस का विषय है कि उन्हें भारत के सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से मरणोपरांत भी सम्मानित नहीं किया गया, जबकि उनके नाम की कई बार सिफारिश हुई थी।
व्यक्तित्व और जीवन दर्शन: एक संत का जीवन
मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी आवाज़ की तरह ही अपने व्यक्तित्व में भी अद्वितीय थे। वे बेहद विनम्र, धार्मिक और शांत स्वभाव के इंसान थे। वे संगीत को केवल एक पेशा नहीं, बल्कि साधना मानते थे और अपने प्रत्येक गीत को ईश्वर की भेंट समझते थे। उनकी दरियादिली और साधु जैसा जीवन उनके साथियों और संगीत उद्योग के लोगों को सदा प्रेरित करता रहा। वे दिखावे से दूर, एक सरल और पवित्र जीवन जीते थे।
मृत्यु और विरासत: अमर स्वर की गूंज
31 जुलाई 1980 को, महज 55 वर्ष की आयु में, मोहम्मद रफ़ी साहब हृदयगति रुकने से इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी अंतिम यात्रा में लगभग 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए, जो अपने प्रिय गायक को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़े थे। मुंबई में भारी बारिश के बीच भी, यह जनसैलाब रफ़ी साहब के प्रति लोगों के अथाह प्रेम और उनके असाधारण प्रभाव का प्रतीक था।
उनकी भौतिक अनुपस्थिति के बावजूद, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आज भी जीवित है।
निष्कर्ष
मोहम्मद रफ़ी केवल गायक नहीं थे, वे भारतीय आत्मा की आवाज़ थे। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास, अपनापन और संवेदनशीलता थी जो पीढ़ियों को जोड़ती है और हर उम्र के श्रोताओं को अपनी ओर खींचती है। आज भी उनके गीत रेडियो, यूट्यूब, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और हर भारतीय के दिलों में गूंजते हैं – वे कभी पुराने नहीं होते, बल्कि हर दिन नए लगते हैं।
उनका जीवन एक आदर्श है – विनम्रता, साधना, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का। रफ़ी साहब की आवाज़ भारतीय सांस्कृतिक विरासत की एक अनमोल धरोहर है, जिसे युगों-युगों तक याद किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ इससे प्रेरणा लेती रहेंगी।
"रफ़ी मर सकता है, उसकी आवाज़ नहीं। वो आज भी ज़िंदा है – हर दिल में, हर धुन में।"
मोहम्मद रफ़ी साहब को शत-शत नमन।















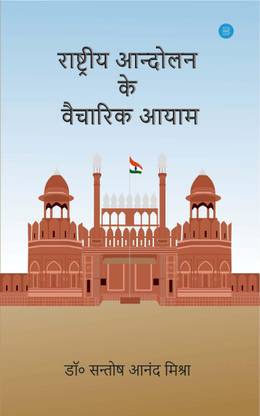





0 Comments
Thank you