राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त: भारतीय चेतना के अमर गायक(3 अगस्त 1886- 12 दिसंबर 1964)
परिचय
हिंदी साहित्य के गौरव, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। वे मात्र एक कवि नहीं, बल्कि एक युग-निर्माता थे, जिनकी लेखनी ने देशवासियों के हृदयों में राष्ट्रप्रेम की ज्योति प्रज्वलित की। महात्मा गांधी ने उन्हें 'राष्ट्रकवि' की उपाधि से विभूषित कर उनके योगदान को अमर कर दिया। गुप्त जी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव, सामाजिक चेतना और नारी सशक्तिकरण का संदेश जन-जन तक पहुँचाया।
जीवन यात्रा: झाँसी के चिरगाँव से राष्ट्रकवि तक
मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले के चिरगाँव में हुआ था। उनके पिता रामचरण कनकने स्वयं एक सहृदय कवि थे, जिनसे गुप्त जी को साहित्यिक संस्कार विरासत में मिले। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहाँ उन्होंने संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन किया। बचपन से ही उनकी काव्य प्रतिभा मुखर होने लगी थी। उनके छोटे भाई सियारामशरण गुप्त भी एक प्रसिद्ध लेखक बने। ऐसे समय में, जब देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा था और समाज में रूढ़िवादिता का बोलबाला था, गुप्त जी ने अपनी कलम को राष्ट्र की पीड़ा का स्वर बना दिया। वे खड़ी बोली हिंदी के पहले सफल कवि माने जाते हैं, जिन्होंने ब्रजभाषा की परंपरा से बाहर निकलकर हिंदी कविता को एक नई दिशा दी।
साहित्यिक यात्रा और 'खड़ी बोली' का उद्भव
गुप्त जी की साहित्यिक यात्रा का आरंभ ब्रजभाषा में हुआ, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। उनकी पहली महत्त्वपूर्ण रचना 'रंग में भंग' (1909) थी। इसके बाद तो उनकी कलम से एक से बढ़कर एक कालजयी रचनाएँ निकलीं। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास और पौराणिक कथाओं को इस तरह से गढ़ा कि वे आधुनिक संदर्भों से जुड़ गईं।
काव्य की विशेषताएँ: एक विराट सोच का दर्पण
गुप्त जी के काव्य में कई अनूठी विशेषताएँ हैं, जो उन्हें अन्य कवियों से अलग करती हैं:
* राष्ट्रीय भावना और देशप्रेम: उनकी कविताओं में राष्ट्रप्रेम का गहरा भाव मिलता है। 'भारत भारती' (1912) इस भावना का सबसे सशक्त उदाहरण है, जिसमें भारत के गौरवशाली अतीत, वर्तमान की दयनीय स्थिति और भविष्य के लिए प्रेरणा का भाव मुखरित होता है।
* नारी चेतना का उत्थान: गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में उपेक्षित और गौण माने गए स्त्री पात्रों को प्रमुखता दी। 'साकेत' में उन्होंने उर्मिला की विरह-व्यथा को केंद्र में रखा, वहीं 'यशोधरा' में बुद्ध की पत्नी यशोधरा के त्याग और पीड़ा को स्वर दिया। यह उनकी नारी के प्रति गहरी संवेदना का परिचायक है।
* पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों का आधुनिक प्रस्तुतिकरण: उन्होंने रामायण, महाभारत और अन्य ऐतिहासिक कथाओं को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। 'जयद्रथ वध', 'साकेत' और 'पंचवटी' जैसी रचनाओं में उन्होंने इन कथाओं को आधुनिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ा।
* सरल, प्रवाहमयी भाषा: उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी, जो सहज, सरल और गंभीर भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम थी। उनकी रचनाएँ जनसाधारण के लिए भी सुगम थीं, जिससे वे बड़ी संख्या में पाठकों तक पहुँचीं।
* सामाजिक समरसता: उन्होंने अपने काव्य में मानवता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया।
प्रमुख कृतियाँ: भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि
गुप्त जी की रचनाएँ भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं।
* 'भारत भारती' (1912): यह वह रचना है जिसने उन्हें 'राष्ट्रकवि' की उपाधि का सच्चा हकदार बनाया। इस ग्रंथ ने स्वतंत्रता सेनानियों में नई ऊर्जा का संचार किया और ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित भी कर दिया था।
* 'साकेत' (1931): महाकाव्य 'साकेत' में गुप्त जी ने राम-कथा को उर्मिला के दृष्टिकोण से लिखा, जिससे हिंदी साहित्य में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ।
* 'यशोधरा' (1932): यह काव्य गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण (गृहत्याग) के बाद उनकी पत्नी यशोधरा की मनोदशा को चित्रित करता है।
* 'जयद्रथ वध': इसमें महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग का वर्णन है, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु और अर्जुन द्वारा जयद्रथ का वध शामिल है।
* अन्य रचनाएँ: 'पंचवटी', 'सिद्धराज', 'कर्ण' आदि भी उनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं।
सम्मान और निधन
मैथिलीशरण गुप्त को उनके अद्भुत साहित्यिक योगदान के लिए कई सम्मान मिले। महात्मा गांधी द्वारा 'राष्ट्रकवि' की उपाधि, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण (1954) का सम्मान और वर्ष 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में उनका योगदान स्मरणीय है। 12 दिसंबर 1964 को इस महान कवि का निधन हो गया। लेकिन उनकी रचनाएँ आज भी जीवित हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
निष्कर्ष
मैथिलीशरण गुप्त केवल एक कवि नहीं, बल्कि एक युग-निर्माता और भारतीय चेतना के सच्चे संवाहक थे। उन्होंने अपनी कलम से सोए हुए राष्ट्र को जगाया, नारी को सम्मान दिया और खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके साहित्य में राष्ट्रप्रेम, सांस्कृतिक गौरव, सामाजिक सुधार और मानवीय मूल्यों का सुंदर संगम मिलता है। उनकी पंक्तियाँ — "नर हो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो" — आज भी हमें जीवन में कर्मठता और आशा का संदेश देती हैं। वे वास्तव में उस भारत के कंठ स्वर थे, जो स्वतंत्रता से पहले विवश था, परंतु सपनों से भरा हुआ था।














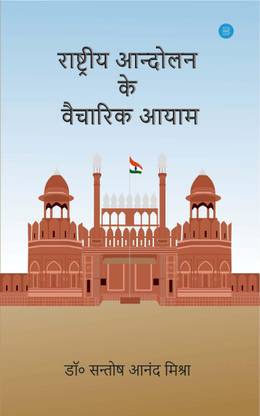





0 Comments
Thank you