जलियांवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल 1919)
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत का राजनीतिक वातावरण
1919 का भारत असंतोष और असुरक्षा की चपेट में था। एक ओर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर भाग लिया था, दूसरी ओर देशवासियों को उम्मीद थी कि इस योगदान के बदले उन्हें स्वशासन या किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत—ब्रिटिश सरकार ने रौलेट एक्ट पारित कर दिया।
रौलेट एक्ट (1919):
सर विलियम रौलेट की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश पर यह कानून लाया गया था। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। यह कानून न्याय, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के विरुद्ध था, जिसे महात्मा गांधी ने "काला कानून" कहा।
देशभर में इस कानून का तीव्र विरोध हुआ। पंजाब में इसका सबसे अधिक विरोध देखने को मिला क्योंकि वहाँ पहले से ही सैन्य शासन जैसा माहौल था।
अमृतसर में आंदोलन और नेताओं की गिरफ्तारी
13 अप्रैल 1919 से कुछ दिन पहले, अमृतसर में रौलेट एक्ट के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। दो लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता—डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया और गुप्त रूप से कश्मीर भेज दिया।
इस अन्याय के खिलाफ शहर में व्यापक रोष फैला। लोगों ने प्रदर्शन किए और शांतिपूर्वक विरोध जताने का प्रयास किया। किंतु प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई, जिससे अनेक लोग मारे गए। इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और जलियांवाला बाग में किसी भी प्रकार की सभा पर रोक लगा दी गई—हालाँकि इसकी सूचना आम जनता को स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी।
जलियांवाला बाग: हत्याकांड का स्थल
जलियांवाला बाग, अमृतसर शहर के बीचों-बीच स्थित एक संकीर्ण प्रवेश द्वार वाला बाग था, जिसके चारों ओर ऊँची दीवारें थीं। यहाँ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के अवसर पर हजारों स्त्री-पुरुष, वृद्ध और बच्चे एकत्र हुए थे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे और कुछ रौलेट एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा में भाग लेने।
जनरल डायर की क्रूर योजना:
ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को जब इस सभा की जानकारी मिली, तो वह लगभग 50 सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। उसके पास राइफलधारी सैनिक थे जिनमें से कुछ के पास मशीन गनें भी थीं। बिना किसी चेतावनी के उसने बाग का एकमात्र निकास बंद कर दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि वे भीड़ पर तब तक गोलियाँ चलाएँ जब तक उनकी गोलियाँ खत्म न हो जाएँ।
नरसंहार: मृत्यु और पीड़ा का मंजर
10 मिनट तक चली गोलीबारी में 1650 राउंड गोलियाँ चलाई गईं। वहाँ उपस्थित लोग भागने के लिए दीवारें चढ़ने लगे, कुछ एकमात्र संकरे रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगे, जबकि अनेक लोग वहीं जमीन पर गिर पड़े। बाग में स्थित कुएँ में लगभग 120 से अधिक लोगों ने जान बचाने के लिए छलाँग लगा दी, लेकिन वे वहीं मर गए।
सरकारी आंकड़े:
ब्रिटिश सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1100 घायल हुए।
भारतीय नेताओं और चश्मदीदों के अनुसार: 1000 से अधिक लोग मारे गए।
देश-विदेश में प्रतिक्रिया
इस भयावह कांड ने संपूर्ण देश को झकझोर दिया।
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना ‘सर’ (नाइटहुड) का खिताब लौटा दिया और ब्रिटिश क्राउन से अलग होने का प्रतीकात्मक विरोध जताया।
- महात्मा गांधी, जो अभी तक ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, उन्होंने यह विश्वास खो दिया और पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में संघर्ष का संकल्प लिया।
- नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे नेता इस हत्याकांड से बहुत आहत हुए और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और तीव्र हो गई।
ब्रिटेन में प्रतिक्रिया:
हालाँकि ब्रिटिश संसद में इस कांड की आलोचना हुई, लेकिन कुछ अंग्रेजों ने डायर का समर्थन किया। उसे अंततः ब्रिटिश सेना से सेवानिवृत्त किया गया, लेकिन उसे दंडित नहीं किया गया।
हंटर आयोग और न्याय का मजाक
ब्रिटिश सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया, जिसे हंटर आयोग कहा गया। इस आयोग ने जनरल डायर से पूछताछ की, और उसने स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य 'भीड़ को सबक सिखाना' था।
हालांकि आयोग ने डायर की कार्रवाई को "गलत" कहा, फिर भी कोई कठोर दंड नहीं दिया गया। यह जांच और न्याय की प्रक्रिया भारतीयों के लिए केवल औपचारिकता बनकर रह गई।
अमर बलिदान: साहित्य, कला और स्मारक में
- जलियांवाला बाग आज एक राष्ट्रीय स्मारक है, जहाँ शहीदों की याद में एक लौ सदा जलती रहती है।
- दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। कुआँ जहाँ लोग कूदे थे, अब भी संरक्षित है।
- इस घटना ने साहित्यकारों, चित्रकारों और फिल्मकारों को भी प्रभावित किया। इसके संदर्भ खुशवंत सिंह के उपन्यासों, सुभद्राकुमारी चौहान और रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की कविताओं में मिलते हैं।
जलियांवाला बाग नरसंहार केवल एक भयानक त्रासदी नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह मोड़ है जहाँ भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के साथ किसी भी प्रकार के समझौते की आशा छोड़ दी। यह घटना सिखाती है कि आजादी के रास्ते में कितने निर्दोषों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
यह बाग आज भी हर भारतीय को याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी यूँ ही नहीं मिली—इसके पीछे बलिदानों की एक लम्बी श्रृंखला है।








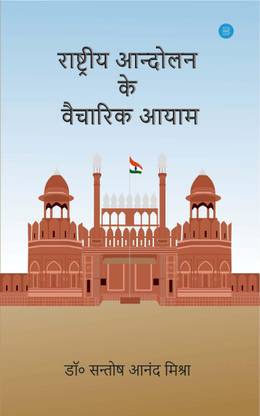



0 Comments
Thank you