डॉ॰ भीमराव अंबेडकर: भारत के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत
भूमिका
भारत जैसे विविधतापूर्ण और ऐतिहासिक रूप से सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त देश में डॉ॰ भीमराव अंबेडकर का उदय एक क्रांतिकारी घटना थी। वे न केवल स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि एक विचारक, समाज सुधारक, राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री, और दलित चेतना के अग्रदूत भी थे। उनका जीवन संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति यदि शिक्षा, आत्मबल और दृढ़ इच्छाशक्ति से सुसज्जित हो, तो वह समाज की सबसे गहरी जड़ों तक परिवर्तन पहुँचा सकता है।
जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि
डॉ॰ भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महू नगर छावनी में हुआ। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की चौदहवीं संतान थे। उनका परिवार मराठी भाषी था और 'महार' जाति से संबंधित था, जिसे उस समय अस्पृश्य माना जाता था। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत थे और शिक्षित थे, जिससे भीमराव की शिक्षा में रुचि प्रारंभिक अवस्था से ही विकसित हुई।
बचपन में उन्हें स्कूल में बैठने, पानी पीने और सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार करने से वंचित किया गया। यह भेदभाव उनके मन में गहरे अंकित हुआ और आगे चलकर उनके जीवन का लक्ष्य बन गया—जातिविहीन, समान और न्यायसंगत समाज की स्थापना।
शिक्षा की ऊँचाइयाँ
प्रारंभिक शिक्षा:
- 1897 में बंबई (अब मुंबई) के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश लिया।
- 1907 में वे इस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अपने समुदाय के पहले छात्र बने।
उच्च शिक्षा:
- 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की।
- 1913 में 'बारोदा राज्य छात्रवृत्ति' के तहत कोलंबिया विश्वविद्यालय (अमेरिका) गए।
- वहाँ से उन्होंने 1915 में एम.ए. और 1917 में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की। उनका शोधपत्र "Ancient Indian Commerce" था।
- इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए जहाँ से उन्होंने डी.एससी. की डिग्री प्राप्त की और साथ ही ग्रेज़ इन (Gray's Inn) से बार-एट-लॉ की उपाधि भी प्राप्त की।
डॉ. अंबेडकर भारत के सर्वाधिक शिक्षित और बहुश्रुत व्यक्तित्वों में से एक थे, जिनकी विद्वता को विश्वभर में सम्मान मिला।
सामाजिक आंदोलन और सुधार कार्य
अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष:
-
चवदार तालाब सत्याग्रह (1927): अछूतों को सार्वजनिक जलस्रोतों से जल ग्रहण करने का अधिकार दिलाने के लिए यह आंदोलन महत्त्वपूर्ण था। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ जाकर वहाँ पानी पिया, जिससे समाज में हलचल मच गई।
-
मनुस्मृति दहन (1927): जातिवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले ग्रंथ 'मनुस्मृति' का सार्वजनिक दहन किया गया।
-
नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह (1930): दलितों के लिए मंदिरों के द्वार खोलने की माँग को लेकर यह आंदोलन चलाया गया।
संस्थाओं की स्थापना:
- बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924): यह संस्था दलितों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए काम करती थी।
- मूकनायक (पत्रिका, 1920) और बहिष्कृत भारत (1927): इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर जनमत तैयार किया।
राजनीतिक जीवन
राजनीतिक दलों की स्थापना:
- इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (1936): मजदूरों और दलितों के हक की आवाज़ उठाने वाला राजनीतिक मंच।
- शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (1942): दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए एक और सशक्त संगठन।
ब्रिटिश भारत में भागीदारी:
- वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री रहे (1942–1946)। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के कल्याण, महिलाओं के अधिकार, और औद्योगिक सुधारों में अहम भूमिका निभाई।
संविधान निर्माण में योगदान
स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में डॉ. अंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी संविधान की रचना की जिसमें:
- सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दी गई।
- अस्पृश्यता को पूर्णतः निषिद्ध किया गया।
- अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।
वे यह मानते थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी अत्यंत आवश्यक है।
धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म
डॉ. अंबेडकर मानते थे कि हिन्दू धर्म की जातिप्रथा में दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कई वर्षों तक धर्मग्रंथों का अध्ययन किया और अंततः 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनके साथ लाखों अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।
उन्होंने "बुद्ध और उनका धर्म" नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को तर्कसंगत, वैज्ञानिक और मानवतावादी धर्म के रूप में प्रस्तुत किया।
लेखन और विचार
डॉ. अंबेडकर ने कई ग्रंथों की रचना की जो सामाजिक विज्ञान, धर्म, राजनीति, और अर्थशास्त्र पर आधारित हैं:
- "Annihilation of Caste" – जाति व्यवस्था पर करारा प्रहार।
- "The Problem of the Rupee" – भारतीय मुद्रा पर विश्लेषणात्मक ग्रंथ।
- "Who Were the Shudras?" – शूद्रों की उत्पत्ति पर ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण।
- "Thoughts on Linguistic States" – भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार।
उनकी लेखनी विचारों की स्पष्टता, तर्क और सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत थी।
मृत्यु और विरासत
डॉ. अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। यह दिन 'महापरिनिर्वाण दिवस' के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 1990 में मरणोपरांत ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया।
आज उनका स्मारक "दीक्षा भूमि" और "भीम जन्मभूमि" जैसे स्थान दलित चेतना और सामाजिक न्याय के प्रतीक बन चुके हैं।
डॉ॰ भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय समाज को वैचारिक दृष्टि दी और समानता पर आधारित राष्ट्र की नींव रखी। वे न केवल संविधान के निर्माता थे, बल्कि एक नई सामाजिक क्रांति के सूत्रधार भी थे।
उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं – जब तक समाज में विषमता और भेदभाव रहेगा, तब तक डॉ. अंबेडकर की आवश्यकता बनी रहेगी।
"जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए।" – डॉ. भीमराव अंबेडकर








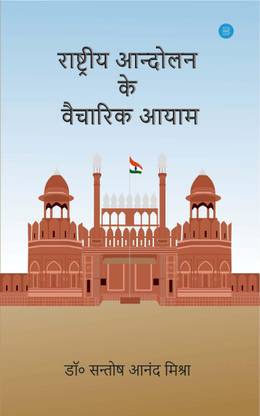



0 Comments
Thank you