मोरारजी देसाई: एक विस्तारपूर्वक दृष्टिकोण
1. परिवार और प्रारंभिक प्रभाव:
मोरारजी देसाई का जन्म एक मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रंचोढ़जी देसाई एक स्कूल शिक्षक थे, जिनका अनुशासनप्रिय स्वभाव मोरारजी के चरित्र में स्पष्ट रूप से झलकता है। उनका लालन-पालन अत्यंत सादगीपूर्ण वातावरण में हुआ, जहाँ नैतिक मूल्यों और शिक्षा को सर्वोच्च माना जाता था। बाल्यावस्था से ही वे आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण के अनुयायी रहे।
2. प्रशासनिक जीवन की शुरुआत:
स्नातक की शिक्षा के बाद वे बॉम्बे प्रांतीय सिविल सेवा में चयनित हुए और डिप्टी कलेक्टर बने। लेकिन जल्द ही उन्हें यह महसूस हुआ कि ब्रिटिश शासन की कठोर और अन्यायपूर्ण नीतियों के अंतर्गत कार्य करना उनके मूल्यों के विरुद्ध है। उन्होंने 1930 में यह नौकरी त्याग दी और गांधीजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए।
3. गांधीवादी जीवनशैली और आत्मसंयम:
मोरारजी देसाई न केवल गांधीजी के अनुयायी थे बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में संपूर्णता से उतारने का प्रयास करते रहे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी विलासिता को छूने नहीं दिया। नियमित योगाभ्यास, ब्रह्मचर्य का पालन, और प्राकृतिक चिकित्सा में आस्था उनके जीवन के अभिन्न अंग थे।
वे "मूत्रचिकित्सा" (urine therapy) के खुले समर्थक थे और मानते थे कि यह शरीर को शुद्ध और रोगमुक्त रखती है। इस पर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मान्यताओं से समझौता नहीं किया।
4. स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका:
- नमक सत्याग्रह (1930): इसमें भाग लेने के कारण उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा।
- भारत छोड़ो आंदोलन (1942): इस आंदोलन में उन्होंने बढ़-चढ़ कर भाग लिया और लंबे समय तक जेल में रहे।
इस दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया।
5. बॉम्बे राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में:
1952 में मोरारजी देसाई बॉम्बे राज्य (वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात) के मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल बेहद सख्त अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता है।
- सरकारी अधिकारियों में जवाबदेही बढ़ाई।
- भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण।
- शिक्षा और वित्तीय मामलों में कई सुधार किए।
उनकी कठोर कार्यशैली से कुछ लोग असहमत भी रहते थे, परंतु उनके कार्यों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वमान्य थी।
6. केंद्रीय राजनीति में योगदान:
वित्त मंत्री के रूप में (1958–1963):
- टैक्स सुधार लागू किए।
- वित्तीय घाटा कम करने के लिए कठोर कदम उठाए।
- रुपया का अवमूल्यन करने से मना कर दिया (हालांकि बाद में यह हुआ)।
गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री (1967–1969):
- इंदिरा गांधी की कुछ नीतियों से मतभेद हुआ, विशेषकर बैंक राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स हटाने के मुद्दे पर।
- इसी मतभेद ने कांग्रेस पार्टी में विभाजन को जन्म दिया। मोरारजी देसाई 'कांग्रेस (ओ)' के प्रमुख नेता बने।
7. प्रधानमंत्री के रूप में प्रमुख निर्णय:
मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्रित्व काल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। इस काल को लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का काल कहा जा सकता है।
- शाह आयोग की स्थापना: आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों की जांच के लिए।
- मीडिया की स्वतंत्रता बहाल की गई।
- संविधान संशोधन: आपातकाल जैसे कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु।
- विदेश नीति: पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में सुधार की कोशिशें। विशेष रूप से पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक के साथ संबंधों को सुधारने के लिए उन्हें 'निशान-ए-पाकिस्तान' पुरस्कार मिला।
परंतु जनता पार्टी के घटक दलों के बीच मतभेद और सत्ता संघर्ष के कारण सरकार अधिक समय नहीं चल सकी। चारु मजूमदार और अन्य वामपंथी विचारकों के दबाव में कुछ नीतिगत निर्णय विवादास्पद भी साबित हुए।
8. आलोचनाएं और विवाद:
- उनका अत्यधिक कठोर प्रशासनिक दृष्टिकोण कभी-कभी उन्हें 'तानाशाही' के रूप में प्रस्तुत करता था।
- मूत्रचिकित्सा को लेकर उपहास भी किया गया।
- इंदिरा गांधी के खिलाफ कड़े कदमों को कुछ लोगों ने व्यक्तिगत प्रतिशोध माना।
लेकिन इन सबके बावजूद, उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता को कभी प्रश्नांकित नहीं किया जा सका।
9. जीवन के अंतिम वर्ष:
प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। वे मुंबई में एक साधारण जीवन व्यतीत करते रहे। 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। वे लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहे—उनके दीर्घजीवी होने का श्रेय वे योग, ब्रह्मचर्य और प्राकृतिक जीवनशैली को दैत्य
मोरारजी देसाई भारतीय राजनीति के उस युग के प्रतिनिधि थे जहाँ सिद्धांतों को राजनीति से ऊपर माना जाता था। वे एक ऐसे नेता थे जिनके पास सत्ता थी, लेकिन सत्ता के लोभ से वे मुक्त थे। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीतिक निर्णय नहीं लिए। उनका जीवन आज भी एक उदाहरण है कि कैसे नैतिक मूल्यों के साथ राजनीति की जा सकती है।








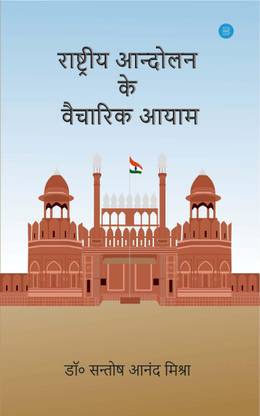



0 Comments
Thank you