भिखारी ठाकुर: लोककलाओं और भोजपुरिया संस्कृति के अमर प्रवक्ता(18 दिसंबर 1887- 10 जुलाई 1971)
भोजपुरी लोक-संस्कृति के अप्रतिम पुरोधा, रंगमंच के महानायक और सामाजिक चेतना के उद्घोषक भिखारी ठाकुर (1887–1971) को "भोजपुरी के शेक्सपीयर" कहा जाता है. उन्होंने अशिक्षित, उपेक्षित और पीड़ित समाज के दुख-दर्द को मंच पर स्वर दिया और सामाजिक सुधार की आवाज को भोजपुरी लोकभाषा में जन-जन तक पहुंचाया.
परिचय
भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में एक नाई परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम दिनबंधु ठाकुर था. आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार में जन्म लेने के कारण वे औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन उनमें ज्ञान की तीव्र ललक थी. बचपन से ही वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और बाल-नाटकों, लोकगीतों और रामलीला के प्रति विशेष आकर्षण रखते थे.
कलात्मक यात्रा की शुरुआत
भिखारी ठाकुर ने अपने जीवन के प्रारंभिक समय में जीविकोपार्जन के लिए कलकत्ता (अब कोलकाता) का रुख किया, जहां उन्होंने नाई का काम किया. हालांकि, उनकी रुचि साहित्य, गीत-संगीत और रंगमंच में अधिक थी. कलकत्ता में ही उन्होंने पढ़ना-लिखना सीखा और नाट्यकला की बारीकियों को आत्मसात किया.
बाद में वे अपने गांव लौटे और एक लोकनाट्य मंडली (नाच पार्टी) की स्थापना की, जिसने गरीब, दलित और मजदूरों के जीवन की वास्तविकताओं को गीतों, संवादों और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया.
भिखारी ठाकुर की प्रमुख रचनाएँ
भिखारी ठाकुर ने गीत, कविता, नाटक और लोकगाथाओं की रचना की. उनके नाटकों में सामाजिक सरोकार, व्यंग्य, करुणा और सुधार का स्वर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.
प्रमुख नाट्य-रचनाएँ:
* बिदेसिया: प्रवासी मजदूरों की पीड़ा पर आधारित.
* गबर घिचोर: सौतेले रिश्तों और पारिवारिक विघटन पर आधारित.
* बेटी बेचवा: दहेज प्रथा और बालविवाह पर तीखा प्रहार.
* नटवा-नच: नाचनेवाले पुरुषों के शोषण को उजागर करता है.
* कलियुग प्रेम: सामाजिक पतन और नैतिकता की गिरावट पर व्यंग्य.
* पुत्र वध: नई पीढ़ी द्वारा माता-पिता की उपेक्षा का चित्रण.
लोकगीत और कविताएँ:
* बिदेसिया गीत
* कजरी, बिरहा, चौताल
* नारी-विमर्श से जुड़े लोकगीत
उनकी भाषा लोकजीवन की सजीव अभिव्यक्ति है - सहज, सरस और भावपूर्ण.
नाट्यशैली और प्रस्तुतिकरण
भिखारी ठाकुर की नाट्यशैली विशिष्ट थी. उन्होंने मंच को सामाजिक जागरूकता का औजार बनाया. उनके नाटकों में गीत, संवाद, नृत्य और व्यंग्य का अनोखा संगम था. उनकी मंडली गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करती थी और जनसामान्य को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती थी. उनकी प्रस्तुतियां भोजपुरी संस्कृति, स्त्री-पुरुष संबंध, प्रवासी मजदूरी, जाति व्यवस्था, दहेज प्रथा और शराबबंदी जैसे विषयों पर केंद्रित थीं.
भाषा और शैली
भिखारी ठाकुर की भाषा शुद्ध, सहज और देहाती भोजपुरी है. उन्होंने लोकगीतों की परंपरा को अपनाया और उसे आधुनिक मंचीय नाट्य रूप दिया. उनकी शैली में हास्य, करुणा, विद्रोह और आध्यात्मिकता का समन्वय देखने को मिलता है.
भिखारी ठाकुर का सामाजिक योगदान
* सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज: बालविवाह, दहेज, स्त्री उत्पीड़न, प्रवासजनित समस्याओं आदि पर उनके नाटकों ने समाज को झकझोर दिया.
* नारी चेतना के संवाहक: उन्होंने स्त्रियों की पीड़ा को प्रमुखता से मंचित किया और उन्हें सामाजिक सम्मान देने की बात कही.
* भोजपुरी की गरिमा में वृद्धि: उन्होंने भोजपुरी को केवल लोकभाषा से उठाकर साहित्यिक और रंगमंचीय भाषा बना दिया.
सम्मान और विरासत
हालांकि भिखारी ठाकुर को उनके जीवनकाल में पर्याप्त सरकारी मान्यता नहीं मिली, लेकिन लोकमान्यता में वे अत्यंत पूज्य बने रहे. आज भी उनकी रचनाएं लोकनाट्य मंडलियों द्वारा मंचित की जाती हैं.
उनकी स्मृति में:
* भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया.
* कई विश्वविद्यालयों में उनके नाटकों पर शोध हो चुके हैं.
* उन पर आधारित फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और मंचीय प्रस्तुतियां आज भी होती रहती हैं.
निधन
भिखारी ठाकुर का निधन 10 जुलाई 1971 को हुआ. वे भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं और विचार आज भी जीवित हैं.
उपसंहार
भिखारी ठाकुर न केवल एक कलाकार थे, बल्कि एक सामाजिक चिंतक, सुधारक और लोकसंस्कृति के योद्धा थे. उन्होंने दिखा दिया कि एक साधारण ग्रामीण भी अपनी कला और संवेदनशीलता से समाज को दिशा दे सकता है. उनका साहित्य हमें हमारी जड़ों की ओर ले जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि "कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि परिवर्तन का माध्यम है."











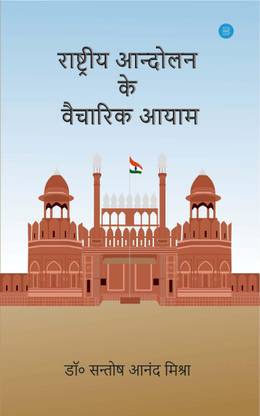





0 Comments
Thank you