डॉ. विक्रम साराभाई: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक(12 अगस्त 1919- 30 दिसंबर 1971)
प्रस्तावना
कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि भविष्य की दिशा तय करते हैं। डॉ. विक्रम अंबालाल साराभाई भारतीय विज्ञान जगत के ऐसे ही एक उज्ज्वल नक्षत्र थे, जिन्होंने सीमित संसाधनों और अनंत सपनों के बीच की दूरी को मिटा दिया। उन्हें केवल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहना पर्याप्त नहीं, क्योंकि उन्होंने भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास की नींव को अपने दूरदर्शी विचारों से सींचा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के बल पर एक राष्ट्र अपनी सीमाओं से परे जाकर नई ऊँचाइयों को छू सकता है।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: एक दूरदर्शी बचपन
जन्म: 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, गुजरात के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में जन्मे विक्रम साराभाई को बचपन से ही प्रगतिशील विचारों का वातावरण मिला। पिता अंबालाल साराभाई और माता सरला देवी साराभाई ने उनमें शिक्षा और समाज सेवा के प्रति गहरी रुचि जगाई।
उनकी शिक्षा की शुरुआत अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज से हुई, जिसके बाद वे 1940 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (St. John’s College) से प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री लेने इंग्लैंड चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब दुनिया उथल-पुथल में थी, वे भारत लौट आए और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) में महान वैज्ञानिक सर सी. वी. रमण के मार्गदर्शन में ब्रह्मांडीय किरणों पर शोध किया। यह वही समय था जब विज्ञान के प्रति उनकी लगन और गहरा गई। 1947 में अपनी पीएच.डी. पूरी करने के बाद वे वापस भारत लौटे, लेकिन उनके मन में एक सपना था - भारत को विज्ञान के शिखर पर ले जाना।
वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक योगदान: एक विशाल वृक्ष की नींव
भौतिकी और अनुसंधान का पालना:
विक्रम साराभाई की सबसे बड़ी उपलब्धि 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (Physical Research Laboratory – PRL) की स्थापना थी। यह केवल एक प्रयोगशाला नहीं, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान का "पालना" बनी। यहाँ उन्होंने ब्रह्मांडीय किरणों, अंतरिक्ष भौतिकी और सौर-भूभौतिकी पर महत्वपूर्ण शोध किए। उनका मानना था कि विज्ञान केवल विदेशी तकनीकों का अनुसरण करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी चुनौतियों का समाधान खुद खोजना होगा।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जन्म:
डॉ. साराभाई की दूरदृष्टि का ही परिणाम था कि भारत ने 1960 के दशक में अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने डॉ. होमी भाभा के साथ मिलकर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1962 में INCOSPAR (Indian National Committee for Space Research) की स्थापना उनकी इसी सोच का नतीजा थी। 1963 में केरल के थुम्बा में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) की स्थापना उनके प्रयासों का ही फल था, जहाँ से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपित हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अंतरिक्ष तकनीक का उद्देश्य केवल सैन्य शक्ति या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन स्तर को सुधारना होना चाहिए। 1969 में उनके नेतृत्व में इसरो (ISRO) की स्थापना हुई, जिसने भारत को एक नया रास्ता दिखाया।
उपग्रह परियोजनाओं का स्वप्न:
डॉ. साराभाई ने ही आर्यभट्ट, भारत के पहले उपग्रह की परिकल्पना की, जिसे उनके निधन के बाद 1975 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। उन्होंने INSAT (Indian National Satellite System) और SITE (Satellite Instructional Television Experiment) जैसी परियोजनाओं का सपना देखा था। SITE के माध्यम से उन्होंने यह कल्पना की थी कि उपग्रहों की मदद से भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा और सूचना को पहुँचाया जा सकता है, जिससे लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा।
संस्थानों की स्थापना: ज्ञान का दीपक
डॉ. साराभाई ने केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना की।
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL), अहमदाबाद (1947)
भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), अहमदाबाद (1961)
न्यूक्लियर साइंस सेंटर, अहमदाबाद
विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर
स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (SAC)
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) की अवधारणा में भी उनका योगदान माना जाता है।
यह सूची उनकी बहुमुखी प्रतिभा और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
दर्शन और दृष्टिकोण: विज्ञान का सामाजिक उद्देश्य
विक्रम साराभाई का दर्शन एक वाक्य में था: "भारत जैसे देश के लिए अंतरिक्ष तकनीक का प्रयोग तभी सार्थक है जब यह सीधे तौर पर आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक हो।" वे विज्ञान को केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि उसे समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ते थे। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जो अपनी तकनीक का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करता है।
पुरस्कार, सम्मान और एक दुखद अंत
अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें 1966 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके निधन के बाद, 1972 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया।
30 दिसंबर 1971 को, केवल 52 वर्ष की आयु में, डॉ. साराभाई का त्रिवेंद्रम (केरल) में अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने भारतीय विज्ञान जगत को एक गहरा सदमा दिया, क्योंकि उस समय वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर थे।
विरासत: एक अमर ज्योति
डॉ. विक्रम साराभाई की विरासत आज भी जीवित है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) और अहमदाबाद में विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर उनके नाम पर हैं। सबसे हाल का सम्मान चंद्रयान-2 के लैंडर को "विक्रम" नाम देना था, जो उनके सपनों को चाँद की सतह पर उतारने जैसा था।
निष्कर्ष
डॉ. विक्रम साराभाई का जीवन एक प्रेरणास्रोत है। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि विज्ञान, जब सही दिशा और मानवीय दृष्टिकोण से संचालित हो, तो वह एक राष्ट्र का भाग्य बदल सकता है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी और यह सुनिश्चित किया कि इस तकनीक का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहकर पूरे देश तक पहुँचे। उनका व्यक्तित्व, कार्य और दूरदर्शिता आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव एक प्रकाश-स्तंभ की तरह रहेगी।

















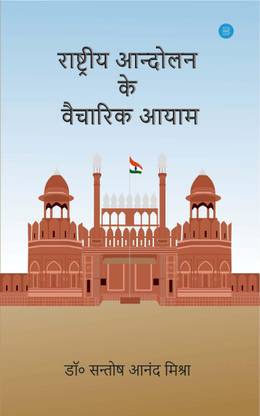





0 Comments
Thank you