भारतीय जनसंघ (Bharatiya Jana Sangh): भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उद्घोषक
परिचय: वैचारिक राजनीति का उदय
भारतीय जनसंघ (BJS) भारतीय गणराज्य के इतिहास में एक ऐसा वैचारिक और ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसने स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय राजनीति की दिशा को स्थायी रूप से प्रभावित किया। 21 अक्टूबर 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित यह दल, राष्ट्रीय एकता, भारतीय संस्कृति और परंपरा को अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनाने वाला पहला प्रमुख राजनीतिक संगठन था। जनसंघ ने न केवल तत्कालीन कांग्रेस के लगभग एकाधिकार वाली राजनीति के सामने एक प्रबल वैचारिक विकल्प प्रस्तुत किया, बल्कि आगे चलकर इसने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विशाल वटवृक्ष की नींव भी रखी, जो आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। यह दल केवल सत्ता का आकांक्षी नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र-निर्माण का एक आंदोलन था।
स्थापना की पृष्ठभूमि: वैचारिक शून्यता को भरना
1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन की त्रासदी हुई, जिसने धार्मिक आधार पर देश को बाँटा। इस पृष्ठभूमि में, स्वतंत्रता के बाद की भारतीय राजनीति पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगभग पूर्ण प्रभुत्व था।
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो स्वयं स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे, ने जल्द ही महसूस किया कि कांग्रेस की नीतियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा, कश्मीर मुद्दे, और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के प्रति उदासीन थीं। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा में पश्चिमी समाजवाद और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का प्रभाव अधिक था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवकों और चिंतकों ने महसूस किया कि भारतीय राजनीति को स्वदेशी, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा, और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मजबूत राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है। इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देने के लिए, डॉ. मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की।
संस्थापक और वैचारिक कर्णधार
जनसंघ की शक्ति उसके नेताओं की विद्वत्ता, त्याग और संगठनात्मक क्षमता में निहित थी:
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी - संस्थापक अध्यक्ष, प्रखर राष्ट्रवादी और 'एक देश, एक विधान' के पहले प्रणेता। उनका बलिदान (1953 में कश्मीर में) जनसंघ के लिए प्रेरणा स्रोत बना।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय - जनसंघ के महासचिव और 'एकात्म मानव दर्शन' (Integral Humanism) के प्रणेता। उन्हें जनसंघ का सर्वोच्च वैचारिक स्तंभ माना जाता है। |
अटल बिहारी वाजपेयी - प्रखर वक्ता, सांसद, और जनसंघ के प्रमुख युवा चेहरा। बाद में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। |
लालकृष्ण आडवाणी - संगठन को सशक्त करने वाले प्रमुख नेता, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के उदय के मुख्य शिल्पकार बने। |
बलराज मधोक, नानाजी देशमुख - प्रमुख संगठनकर्ता और वैचारिक प्रचारक।
मूल विचारधारा: संस्कृति, दर्शन और राष्ट्रवाद
भारतीय जनसंघ की विचारधारा को निम्नलिखित तीन प्रमुख स्तंभों के माध्यम से समझा जा सकता है, जो इसे तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य से विशिष्ट बनाते थे:
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Cultural Nationalism)
जनसंघ का मानना था कि भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई या राज्यों का संघ नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में देखा जाना चाहिए। यह राष्ट्रवाद भारत की सनातन परंपराओं, साझा मूल्यों और इतिहास में निहित है। उन्होंने राष्ट्र की पहचान को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अविभाज्य माना।
एकात्म मानव दर्शन (Integral Humanism)
यह दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा 1965 में प्रतिपादित किया गया, जो जनसंघ की आर्थिक और सामाजिक नीति का आधार बना।
यह दर्शन पूँजीवाद (Capitalism) और साम्यवाद (Communism) दोनों के भौतिकवादी चरम को अस्वीकार करता था। इसका लक्ष्य व्यक्ति, समाज, प्रकृति और राष्ट्र के बीच समन्वय स्थापित करते हुए, मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समग्र विकास करना था।
भारतीयकरण (Indianization)
जनसंघ ने आग्रह किया कि देश की नीतियाँ, शिक्षा पद्धति, प्रशासन और आर्थिक मॉडल भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित होने चाहिए, न कि पश्चिमी विचारधाराओं की नकल पर। इसका अर्थ था राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च रखना और स्वदेशी समाधानों को प्राथमिकता देना।
मुख्य नीतियाँ और आंदोलन
जनसंघ ने जिन प्रमुख नीतियों पर ज़ोर दिया, वे भारतीय राजनीति की मूल धारा को चुनौती देती थीं:
कश्मीर और अनुच्छेद 370: जनसंघ का सबसे प्रसिद्ध आंदोलन अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और कश्मीर के पूर्ण विलय की मांग थी। डॉ. मुखर्जी ने "एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे" का ऐतिहासिक नारा दिया और इसी उद्देश्य के लिए कश्मीर यात्रा के दौरान उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया (1953)।
गोवंश संरक्षण: गाय को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते हुए गाय और गोवंश संरक्षण की मांग को राजनीतिक पटल पर मजबूती से उठाया।
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना: हिंदी को राष्ट्रीय एकता की कड़ी मानते हुए, इसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने पर बल दिया।
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code): देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून की वकालत की।
आर्थिक नीति: आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन, और विकेंद्रीकृत आर्थिक विकास पर जोर दिया।
राजनीतिक संघर्ष और विलय
प्रारंभिक चुनाव (1952-1962): शुरुआती चुनावों में जनसंघ को सीमित सफलता मिली (1952 में 3 सीटें, 1957 में 4 सीटें)। इसका आधार मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों और उत्तर भारत (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान) में रहा।
गठबंधन की राजनीति (1967): 1967 के चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व कम हुआ, और जनसंघ ने कई राज्यों में संविद (Samyukta Vidhayak Dal) सरकारों में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पहुँच बढ़ाई।
आपातकाल (1975-1977): इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का जनसंघ ने कड़ा विरोध किया। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी सहित हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल विरोधी संघर्ष ने विरोधी दलों को एकजुट करने का काम किया।
जनता पार्टी का गठन (1977): आपातकाल समाप्त होने पर, जनसंघ ने कांग्रेस के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस (ओ), और अन्य दलों के साथ विलय करके जनता पार्टी का गठन किया, जो पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के रूप में विरासत
जनता पार्टी की एकता अधिक समय तक नहीं टिक सकी। 1980 में, दोहरी सदस्यता (Dual Membership) के मुद्दे (जनसंघ के पूर्व सदस्यों का RSS से जुड़ाव) पर जनता पार्टी टूट गई।
इसी बिखराव के बाद, जनसंघ की मूल विचारधारा को पुनर्जीवित करते हुए, उसके नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गठन किया। इस प्रकार, भारतीय जनसंघ ने अपने वैचारिक रूप को एक अधिक व्यापक, संगठित और सफल राजनीतिक शक्ति में रूपांतरित कर दिया, जिसने आगे चलकर 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन और राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से सत्ता के शिखर को छुआ।
योगदान और महत्व
भारतीय जनसंघ का भारतीय राजनीति में योगदान केवल सीटें जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारधारा के बीजारोपण का प्रतीक है:
राष्ट्रवाद का पुनर्गठन: जनसंघ ने भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा को एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत आयाम दिया, जो आज भी भारतीय राजनीति के केंद्र में है।
वैचारिक विकल्प: इसने कांग्रेस की प्रभुत्व वाली राजनीति में एक गैर-पश्चिमी, भारतीय-केंद्रित वैचारिक ध्रुव का निर्माण किया।
संगठनात्मक शक्ति: RSS की वैचारिक और संगठनात्मक शक्ति का राजनीति में प्रयोग किया, जिससे भविष्य की BJP को एक मजबूत कैडर-आधारित संरचना मिली।
नींव का पत्थर: जनसंघ भारतीय राजनीति में एक ऐसी राजनीतिक शक्ति की प्रेरणा और पृष्ठभूमि है, जिसने 21वीं सदी में भारत के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया।
निष्कर्ष
भारतीय जनसंघ भारतीय राजनीति का वह दीपस्तंभ था, जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और भारतीय मूल्यों पर आधारित राजनीतिक सोच को जन्म दिया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे राजनीतिक मंच प्रदान किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसे एकात्म मानव दर्शन की वैचारिक गहराई दी।
जनसंघ ने 1951 में जो बीज बोया, वही संघर्षों और विलयों के दौर से गुजरते हुए, आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक विशाल वटवृक्ष बना, जिसने भारत की लोकतांत्रिक और वैचारिक संरचना को स्थायी रूप से प्रभावित किया। जनसंघ का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि राष्ट्र के सांस्कृतिक और वैचारिक पुनर्जागरण का भी माध्यम है।
भारतीय जनसंघ का मुख्य नारा:
“एक देश, एक विधान, एक निशान – यही है जनसंघ की पहचान।”









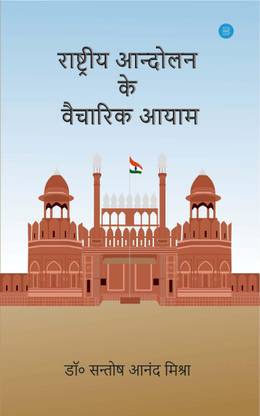





0 Comments
Thank you