बारीन्द्र कुमार घोष: क्रांति और साधना के संगम का अप्रतिम योद्धा
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में असंख्य ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मातृभूमि को दासता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अथक संघर्ष किया। ऐसे ही महान क्रांतिकारियों में एक तेजस्वी नाम है — बारीन्द्र कुमार घोष। वे केवल एक प्रखर क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक ओजस्वी पत्रकार, संवेदनशील लेखक और गहन आध्यात्मिक साधक भी थे। उनके जीवन में देशभक्ति की प्रचंड ज्वाला, त्याग की उदात्त भावना और तपस्या की गहरी त्रिवेणी प्रवाहित होती थी।
प्रारंभिक जीवन एवं सांस्कृतिक प्रभाव
बारीन्द्र कुमार घोष का जन्म 5 जनवरी, 1880 को ब्रिटिश भारत के जेसोर (वर्तमान बांग्लादेश में स्थित) जिले के नरैल नामक स्थान पर हुआ। वे एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक चिंतक और स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता अरविंद घोष (श्री अरविंद) के छोटे भाई थे। उनका परिवार भारतीय नवजागरण काल के अग्रणी विचारकों में गिना जाता था। उनके पिता, कृष्णधन घोष, एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे, जिनकी अंग्रेजी साहित्य और दर्शन में गहरी रुचि थी। उनकी माता, स्वर्णलता देवी, बंगाल में महिला शिक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रबल समर्थक थीं। इस प्रकार, बारीन्द्र का लालन-पालन एक ऐसे प्रगतिशील वातावरण में हुआ, जहाँ पश्चिमी ज्ञान और भारतीय परंपरा का अद्भुत समन्वय था।
उनके बड़े भाई, अरविंद घोष (जिन्हें बाद में श्री अरविंद के नाम से जाना गया), भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आध्यात्मिक और वैचारिक आधारस्तंभ बने। बारीन्द्र ने अपनी क्रांतिकारी चेतना और योग-साधना की प्रारंभिक प्रेरणा उन्हीं से प्राप्त की। पारिवारिक परिवेश ने उनके भीतर राष्ट्रप्रेम और ज्ञान की गहरी नींव रखी।
इंग्लैंड में अध्ययन और भारत वापसी
बारीन्द्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जहाँ वे चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे। किंतु, पश्चिमी सभ्यता का खोखलापन, औपनिवेशिक ठाठ-बाट और भारत में हो रहे शोषण की कटु वास्तविकता ने उन्हें भीतर से उद्वेलित कर दिया। इंग्लैंड में प्रवास के दौरान ही उनकी मुलाकात भारतीय छात्रों के गुप्त राष्ट्रवादी संगठनों के नेटवर्क से हुई। यह अनुभव उनके भावी क्रांतिकारी जीवन की मजबूत नींव बना।
1902 में वे अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत लौट आए और बंगाल की उर्वर भूमि को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांति की प्रयोगशाला बनाने का दृढ़ संकल्प लिया।
अनुशीलन समिति में सक्रिय भागीदारी
अनुशीलन समिति की स्थापना यद्यपि 1902 में हुई थी, लेकिन 1905 के बंग-भंग (बंगाल के विभाजन) के बाद इस संगठन ने तीव्र गति पकड़ी और युवाओं के बीच राष्ट्रप्रेम की लहर दौड़ पड़ी। बारीन्द्र घोष इस क्रांतिकारी संगठन के मुख्य रणनीतिकार और कुशल प्रशिक्षक बनकर उभरे।
उन्होंने बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में गुप्त रूप से युवाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, उन्हें ब्रिटिश गुप्तचरों से बचने की कला सिखाई, बम निर्माण की तकनीकों से अवगत कराया और क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए आवश्यक कूटनीति का पाठ पढ़ाया।
उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ इस प्रकार थीं:
* अनुशीलन समिति के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और संचालन।
* बम निर्माण की गुप्त इकाइयों का गठन, जहाँ क्रांतिकारियों ने हथियार तैयार किए।
* ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की साहसिक योजनाएँ बनाना — जिसमें कुख्यात मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की योजना प्रमुख थी, दुर्भाग्यवश जिसके परिणामस्वरूप कन्हाईलाल दत्त और खुदीराम बोस जैसे वीर क्रांतिकारियों को अपनी शहादत देनी पड़ी।
युगांतर पत्रिका और वैचारिक क्रांति
1906 में ‘युगांतर’ नामक एक अत्यंत प्रभावशाली क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन बारीन्द्र घोष के नेतृत्व में आरंभ हुआ। यह पत्रिका शीघ्र ही माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले युवाओं का उद्घोष बन गई। इसके ज्वलंत लेखों में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों की तीखी आलोचना की जाती थी, युवाओं से हथियार उठाकर स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष करने की अपील की जाती थी, और भारत के गौरवशाली इतिहास की प्रेरणादायक कहानियाँ प्रकाशित की जाती थीं।
‘युगांतर’ के कुछ प्रमुख और उत्तेजक लेखों ने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी और बारीन्द्र घोष को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे ख़तरनाक क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों में से एक माना जाने लगा। इस पत्रिका ने बंगाल के युवाओं में देशभक्ति की एक नई लहर पैदा की और उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
अलीपुर बम केस: क्रांतिकारिता की कसौटी
1908 में, क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर बम से हमला करने की एक योजना बनाई, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने बंगाल में व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियाँ शुरू कर दीं। बारीन्द्र घोष और उनके बड़े भाई श्री अरविंद दोनों पर राजद्रोह और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का मुकदमा चलाया गया, जो ब्रिटिश भारत के इतिहास का सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण मामला बन गया — “अलीपुर बम केस”।
अभियोजन पक्ष ने इस सनसनीखेज मामले में कुल 48 अभियुक्तों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। बारीन्द्र घोष को इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार माना गया और उन्हें ब्रिटिश न्यायपालिका द्वारा फांसी की कठोर सजा सुनाई गई, जिसे बाद में जन दबाव और कानूनी प्रक्रियाओं के चलते आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इस मुकदमे में श्री अरविंद को प्रसिद्ध वकील चितरंजन दास की कुशल वकालत के कारण निर्दोष साबित किया गया।
अंडमान का जीवन: आत्मा की साधना
बारीन्द्र को अंडमान के कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे ‘काला पानी’ के नाम से जाना जाता था। यह जेल भारतीय देशभक्तों के लिए एक नरक के समान यातना स्थल थी, जहाँ कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में कठोर श्रम और मानसिक उत्पीड़न सहना पड़ता था। लेकिन बारीन्द्र घोष ने इस अत्यंत कठिन समय में भी अपने आत्मबल को कमजोर नहीं पड़ने दिया।
अंडमान की काल कोठरियों में उन्होंने:
* गहन योग साधना और ध्यान का नियमित अभ्यास किया, जिससे उन्हें आंतरिक शक्ति और शांति मिली।
* जेल में निरक्षर अन्य कैदियों को शिक्षित करने का प्रयास किया, ज्ञान की ज्योति फैलाने का कार्य जारी रखा।
* भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की दिशा और भविष्य पर गहन आत्मचिंतन में स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दिया।
अंडमान जेल में बिताए गए उनके हृदयविदारक अनुभव बाद में उनकी आत्मकथा ‘The Tale of My Exile’ में विस्तार से सामने आए, जो उस दौर के क्रांतिकारियों की पीड़ा और दृढ़ संकल्प का एक मार्मिक दस्तावेज है।
रिहाई और जीवन का दूसरा अध्याय
1920 में, महात्मा गांधी के प्रभाव से चले सामान्य क्षमादान अभियान के अंतर्गत बारीन्द्र घोष को अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया और अपना शेष जीवन लेखन, सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक साधना के प्रति समर्पित कर दिया।
इस नए चरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार रहा:
* उन्होंने कोलकाता से प्रकाशित होने वाले विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेख लिखे, जिनमें उनके क्रांतिकारी विचारों के साथ-साथ सामाजिक और आध्यात्मिक चिंतन भी शामिल थे।
* उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत को पुनर्प्रकाशित करने और राष्ट्रीय चेतना को जागृत रखने का अथक प्रयास किया।
* उन्होंने महिलाओं की स्थिति, शिक्षा के महत्व और समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर गंभीर चिंतन किया और अपने विचारों को लेखों के माध्यम से व्यक्त किया।
कुछ समय के लिए वे श्री अरविंद आश्रम (पांडिचेरी) से भी जुड़े रहे, लेकिन उनका स्वभाव स्वतंत्र चिंतन का था, इसलिए वे अपनी आध्यात्मिक राह पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते रहे।
कृतित्व और साहित्यिक योगदान
बारीन्द्र घोष की लेखनी उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का दर्पण थी, जिसमें क्रांतिकारी विचारों की प्रचंडता, गहन आत्मनिरीक्षण की गहराई, वेदांत दर्शन का सार और समाज के प्रति गहरी चेतना का सुंदर संगम देखने को मिलता है।
उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ निम्नलिखित हैं:-
* The Tale of My Exile – यह उनकी आत्मकथा है, जो अंडमान जेल के कठोर जीवन का एक जीवंत और हृदयस्पर्शी दस्तावेज है।
* Narir Katha – यह नारी जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनकी सामाजिक स्थिति पर एक गहन विश्लेषणात्मक कृति है।
* Pather Ingit – यह सामाजिक परिवर्तन और प्रगति पर उनके विचारों का एक महत्वपूर्ण लेख संग्रह है।
* Amader Atit (हमारा अतीत) – यह भारतीय इतिहास पर उनकी एक विशिष्ट दृष्टि को प्रस्तुत करने वाली रचना है।
उनकी ये रचनाएँ न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों को प्रकट करती हैं, बल्कि उस युग के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं।
बारीन्द्र घोष की विरासत
बारीन्द्र घोष एक ऐसे असाधारण युग पुरुष थे जिनके व्यक्तित्व में अग्नि (क्रांति की ज्वाला) और आत्मा (आध्यात्मिक गहराई) का एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग था। उन्होंने एक ओर जहाँ युवाओं के हाथों में हथियार थमाकर उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर उन्हें आत्मा की खोज और आत्मचिंतन के गहरे मार्ग पर भी चलने का संदेश दिया।
उनकी अमूल्य विरासत हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि:
* आज़ादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और वैचारिक स्वतंत्रता भी है।
* बाहरी संघर्ष के साथ-साथ आंतरिक आत्मचिंतन और आत्म-सुधार भी उतना ही आवश्यक है।
* इतिहास का निर्माण केवल प्रसिद्ध नेताओं से ही नहीं होता, बल्कि इसमें असंख्य गुमनाम क्रांतिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिनके त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए।
निधन और स्मृति
18 अप्रैल, 1959 को उन्होंने इस भौतिक संसार से विदा ली। वे एक ऐसे युग के साक्षी और निर्माता थे, जिसने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने का स्वप्न देखा और उसे साकार करने के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य योगदान दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत बलिदान होती है और इसके लिए सच्चे मन से संघर्ष करना पड़ता है।
बारीन्द्र कुमार घोष क्रांति और साधना दोनों के प्रतीक हैं। वे न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक अगुआ योद्धा थे, बल्कि भारतीय आत्मा के गहन साधक भी। उनका जीवन भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जिसे आज भी अधिक गहराई से समझा, अध्ययन करने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। उनके बलिदान और उनके चिंतन आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, त्याग और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।









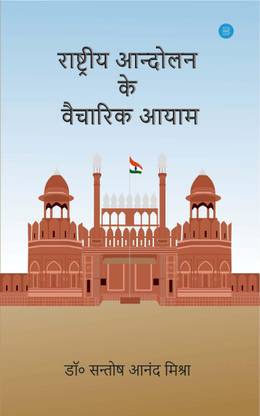



0 Comments
Thank you