सर्वपल्ली राधाकृष्णन: ज्ञान, करुणा और राष्ट्रनिर्माण के अप्रतिम शिल्पी
जीवन का अरुणोदय और पारिवारिक संस्कार
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर, 1888 को तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी के तिरुत्तनी नामक शांत कस्बे में हुआ, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। उनके पिता, सर्वपल्ली वीरस्वामी, राजस्व विभाग में एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी थे, जिनकी गहरी धार्मिक आस्था थी। उनकी माता, सीतानम्मा, एक समर्पित गृहिणी थीं, जिनका हृदय श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण था। उनका परिवार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के "सर्वपल्ली" नामक एक छोटे से गाँव से ताल्लुक रखता था, और इसी पैतृक स्थान ने उनके नाम को स्थायी पहचान दी।
यद्यपि उनके परिवार को आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक बंधनों का सामना करना पड़ा, उनके माता-पिता ने शिक्षा के महत्व को गहराई से समझा था। उन्होंने अपने मेधावी पुत्र राधाकृष्णन को बचपन से ही ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित किया, यह जानते हुए कि शिक्षा ही प्रगति का सच्चा मार्ग है।
ज्ञानार्जन का दुर्गम पथ और प्रज्ञा की दीपशिखा
राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा तिरुत्तनी और तिरुपति के विद्यालयों में हुई। उनकी असाधारण प्रतिभा और ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण ने उन्हें छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जो उनकी शिक्षा के मार्ग में सहायक बनीं। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने दर्शनशास्त्र को अपने मुख्य अध्ययन विषय के रूप में चुना। यह चुनाव मात्र एक संयोग नहीं था, बल्कि उनके एक प्रेरणादायक गुरु और कॉलेज के पुस्तकालय में पढ़ी गई फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रैडली की एक प्रभावशाली कृति का परिणाम था, जिसने उनके बौद्धिक क्षितिज को नई दिशा दी।
अपनी लगन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, उन्होंने 1906 में दर्शनशास्त्र में स्नातक की डिग्री और 1909 में स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। उनका स्नातकोत्तर शोध प्रबंध, "The Ethics of the Vedanta and Its Metaphysical Presuppositions," इतना उत्कृष्ट माना गया कि उसे मद्रास विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के अमूल्य संग्रह में स्थान दिया गया, जो उनकी प्रारंभिक विद्वता का प्रमाण था।
शिक्षण का यज्ञ और बौद्धिक साधना
डॉ. राधाकृष्णन ने 1909 में मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज में एक प्राध्यापक के रूप में अपने यशस्वी शिक्षण जीवन का शुभारंभ किया। अपनी अद्वितीय शिक्षण शैली और गहन ज्ञान के कारण, उन्होंने शीघ्र ही छात्रों के मध्य एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात, उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन कार्य किया, जहाँ उन्होंने न केवल छात्रों को ज्ञान प्रदान किया, बल्कि उनके हृदय में जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच के बीज भी बोए। उन्होंने BHU के उपकुलपति के रूप में भी कुशलतापूर्वक कार्य किया, संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1931 से 1936 तक उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान जारी रखा।
उनकी विद्वता की कीर्ति सीमाओं को लांघकर वैश्विक स्तर पर तब फैली, जब उन्हें 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित "Spalding Professor of Eastern Religions and Ethics" के रूप में नियुक्त किया गया। यह किसी भी भारतीय विद्वान के लिए एक अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने पश्चिमी जगत को भारतीय दर्शन की गहराई से परिचित कराया।
उनका शिक्षण मात्र सूचनाओं का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि यह विद्यार्थियों में विवेक, तर्कशक्ति और एक गहरी आध्यात्मिक चेतना के विकास पर केंद्रित था। उनका मानना था कि एक सच्चा शिक्षक वह नहीं होता जो छात्रों को तैयार उत्तर प्रदान करे, बल्कि वह होता है जो उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न पूछने और ज्ञान की अपनी राह खोजने के लिए प्रेरित करे। उनके शब्द आज भी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं: "सच्चा शिक्षक वह नहीं जो छात्रों को उत्तर दे, बल्कि वह है जो उन्हें सोचने की प्रेरणा दे।"
दार्शनिक चिंतन और भारतीयता की नव व्याख्या
डॉ. राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन को केवल प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन मात्र नहीं माना, बल्कि इसे जीवन को समझने और जीने की एक जीवंत पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। वे अद्वैत वेदांत के एक महान और प्रभावशाली प्रवक्ता के रूप में उभरे, जिन्होंने इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक युग की आवश्यकताओं और समझ के अनुरूप प्रस्तुत किया। उनके दार्शनिक विचारों के अनुसार, ब्रह्म ही परम और अंतिम सत्य है, और प्रत्येक आत्मा उस अनन्त ब्रह्म का ही एक अभिन्न अंश है।
उन्होंने धर्म को बाह्य कर्मकांडों या संकीर्ण मान्यताओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिक खोज और उच्च नैतिक आचरण के रूप में परिभाषित किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य किसी एक विशेष मत की श्रेष्ठता स्थापित करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक मानव के भीतर निहित ईश्वरत्व की अनुभूति कराना है।
उनके प्रमुख दार्शनिक योगदान निम्नलिखित हैं:
* धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव:
उन्होंने सभी धर्मों के मूल सत्य को स्वीकार करते हुए सहिष्णुता और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया।
* तर्क और श्रद्धा का सामंजस्य:
उन्होंने दर्शन में तर्क और बुद्धि के महत्व को स्वीकार करते हुए श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभव के महत्व को भी स्थापित किया।
* भारतीयता और आधुनिकता का समन्वय:
उन्होंने भारतीय दर्शन के शाश्वत मूल्यों को आधुनिक वैज्ञानिक और सामाजिक विचारों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा।
* मानवतावाद और विश्व बंधुत्व की भावना:
उनका दर्शन मानव मात्र की एकता और विश्व शांति के आदर्शों पर आधारित था।
साहित्यिक विरासत: प्रज्ञा के अमूल्य रत्न
डॉ. राधाकृष्णन की लेखनी ने भारतीय दर्शन को विश्व के बौद्धिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी प्रमुख कृतियाँ आज भी दर्शनशास्त्र के छात्रों और विद्वानों के लिए ज्ञान का अक्षय स्रोत हैं:
* Indian Philosophy (दो खंडों में):
भारतीय दर्शन के इतिहास और प्रमुख विचारधाराओं का विस्तृत और गहन विश्लेषण।
* The Hindu View of Life:
हिन्दू धर्म के मूल सिद्धांतों और जीवन दर्शन की सारगर्भित व्याख्या।
* Eastern Religions and Western Thought:
पूर्वी धर्मों और पश्चिमी विचारों के बीच तुलनात्मक अध्ययन, जो आपसी समझ और संवाद को बढ़ावा देता है।
* An Idealist View of Life:
जीवन के आदर्शवादी दृष्टिकोण का दार्शनिक विवेचन।
* The Philosophy of Rabindranath Tagore:
रवींद्रनाथ टैगोर के दार्शनिक विचारों का गहन विश्लेषण।
* Recovery of Faith:
आधुनिक युग में आस्था के महत्व और उसकी पुनर्स्थापना पर विचार।
* Religion and Society:
धर्म और समाज के बीच जटिल संबंधों का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य।
इन महत्वपूर्ण ग्रंथों में, उन्होंने हिन्दू धर्म के मूल तत्वों को एक सुसंगत, तार्किक और बौद्धिक रूप में व्याख्यायित किया, जिससे पश्चिमी जगत को भारतीय चिंतन की गहराई और व्यापकता का परिचय मिला।
राजनीतिक विवेक और राजनयिक कौशल
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, डॉ. राधाकृष्णन ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने हमेशा उच्च नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा। उनकी राजनीतिक यात्रा भी उनके दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रेरित थी।
* 1946-1952: उन्हें सोवियत संघ में भारत के पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इस चुनौतीपूर्ण भूमिका में उन्होंने अपनी कूटनीतिक क्षमता और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
* 1952-1962: उन्होंने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में अपनी विद्वता, निष्पक्षता और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया।
* 1962-1967: वे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा, जिसमें 1962 का भारत-चीन युद्ध और 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध शामिल हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भी उनका संतुलित और परिपक्व नेतृत्व स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने राष्ट्र को एकजुट रखने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
राष्ट्रपति के रूप में, वे मात्र एक औपचारिक प्रमुख नहीं थे, बल्कि राष्ट्र के नैतिक मार्गदर्शक भी थे। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की सच्ची समृद्धि केवल उसकी सैन्य शक्ति या आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस राष्ट्र के नागरिकों के नैतिक चरित्र पर आधारित होती है। उनके शब्द इस सत्य को उजागर करते हैं: "राष्ट्रों की समृद्धि केवल सैन्य बल या आर्थिक विकास से नहीं होती, बल्कि उस राष्ट्र के नागरिकों की नैतिकता से होती है।"
शिक्षक दिवस की अमर परंपरा
जब डॉ. राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, तो उनके पूर्व छात्र और प्रशंसक उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते थे। अपनी स्वाभाविक विनम्रता और शिक्षकों के प्रति गहरे सम्मान के साथ, उन्होंने उत्तर दिया: "मेरे जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने के बजाय यदि इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी।"
उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए, 5 सितंबर को भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने और शिक्षा के महत्व को याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है। यह परंपरा डॉ. राधाकृष्णन के शिक्षा के प्रति अटूट समर्पण और शिक्षकों के प्रति उनके गहरे सम्मान की चिरस्थायी स्मृति है।
सम्मान और उपलब्धियों का गौरव
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया:
* भारत रत्न (1954): भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो उन्हें उनके अद्वितीय विद्वता और राष्ट्र सेवा के लिए प्रदान किया गया।
* टेम्पलटन पुरस्कार: धर्म और मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ।
* ब्रिटिश नाइटहुड: ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई यह उपाधि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी, जो उनकी राष्ट्रीय निष्ठा का प्रतीक है।
* मानद डॉक्टरेट: उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और भारत के कई अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त हुईं, जो उनकी विद्वता का सम्मान थीं।
* यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि: उन्होंने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ये सम्मान उनकी बहुमुखी प्रतिभा, गहन ज्ञान और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के प्रमाण हैं।
देहावसान और स्मृतियों का अनंत प्रवाह
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 17 अप्रैल, 1975 को चेन्नई में अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन से भारत ने न केवल एक पूर्व राष्ट्रपति को खोया, बल्कि एक महान ब्रह्मज्ञानी विचारक, असंख्य विद्यार्थियों के पथप्रदर्शक और मानवता के एक सच्चे पुजारी को खो दिया। उनका जाना भारतीय दर्शन और शिक्षा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी।
ज्ञान, करुणा और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसी विलक्षण विभूति थे, जिनमें गहन विद्वता, सहजता और अद्भुत तेजस्विता का एक दुर्लभ संगम था। वे न केवल भारतीय संस्कृति के एक उत्कृष्ट प्रतिनिधि थे, बल्कि विश्व मंच पर एक नैतिक और दार्शनिक चेतना के प्रकाश स्तंभ के रूप में भी प्रतिष्ठित थे।
उनकी जीवन गाथा हमें यह अनमोल शिक्षा देती है कि शिक्षा मात्र ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास भी है; दर्शन केवल तार्किक विश्लेषण नहीं है, बल्कि आत्मबोध और सत्य की खोज की एक गहन प्रक्रिया है; और राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
उनके जीवन का सार एक सुंदर उपमा में समाहित है: "वह दीपक जो स्वयं जलता है, वही दूसरों को रोशनी देता है – और राधाकृष्णन उस दीपक का नाम थे।" उनकी प्रज्ञा की रोशनी आज भी हमें प्रेरित करती है और उनके आदर्श हमें एक बेहतर भविष्य की ओर मार्गदर्शन करते रहेंगे।








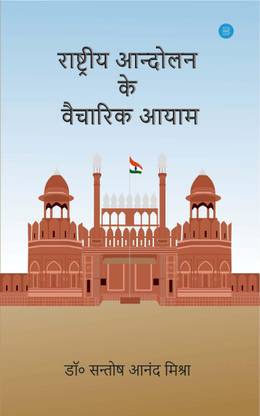



0 Comments
Thank you