वराहगिरी वेंकट गिरी (V. V. Giri) : जीवन, संघर्ष और विरासत(10 अगस्त 1894- 24 जून 1980)
परिचय
वराहगिरी वेंकट गिरी (V. V. Giri) भारत के प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों में से एक थे — एक श्रमिक नेता, स्वतंत्रता सेनानी, कूटनीतिज्ञ और अंततः भारत के चौथे राष्ट्रपति। उनका पूरा नाम Varahagiri Venkata Giri था। वे 10 अगस्त 1894 को बृहत्पुर/बरहामपुर (वर्तमान ओडिशा) में जन्मे और 24 जून 1980 को मद्रास (अब चेन्नै) में निधन हुआ। उन्होंने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया; वे अकेले ऐसे व्यक्ति रहे जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
प्रारम्भिक जीवन और शिक्षा
गिरी का परिवार तेलुगु पृष्ठभूमि से था; उनके पिता वकील और राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। प्रारम्भिक शिक्षा बरहामपुर में हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने ख़ल्लिकोटे कॉलेज से की। 1913–1916 के बीच वे आयरलैंड गए और University College Dublin (UCD) तथा Honourable Society of King’s Inns, Dublin में विधि की पढ़ाई की — वहाँ के समय ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और संगठनात्मक अनुभव दोनों को आकार दिया।
स्वतंत्रता संग्राम और श्रमिक आंदोलन में योगदान
गिरी ने अपने करियर की शुरुआत में ही वैधानिक पेशा छोड़कर गांधीजी के आह्वान पर अहिंसक आन्दोलन में शामिल होना चुन लिया। वे भारत के श्रमिक आंदोलन के अग्रदूतों में रहे — 1923 में उन्होंने All India Railwaymen's Federation के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में AITUC (All India Trade Union Congress) के अध्यक्ष भी बने (प्रथम बार 1926 में और पुनः 1942 में)। 1927 में वे ILO (International Labour Organization) में भारतीय श्रमिक प्रतिनिधि रहे। 1928 में बंगाल-नागपुर रेलवे के मजदूरों के शांतिपूर्ण हड़ताल नेतृत्व को श्रमिक अधिकारों की लड़ाई में मील का पत्थर माना जाता है। इन गतिविधियों के कारण वे बार-बार गिरफ़्तार भी हुए और जेल भी गए।
केंद्रीय राजनीति, 'गिरी दृष्टिकोण' और प्रशासनिक पद
स्वतंत्रता के बाद गिरी ने कई औपचारिक सार्वजनिक पदों पर कार्य किया — 1947–51 तक वे भारत के पहले हाई कमीशनर (High Commissioner) के रूप में सीलोन (अब श्रीलंका) में रहे। 1952 में वे लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और संसदीय कैबिनेट में श्रम मंत्री बने (1952–1954)। मंत्री रहते हुए उन्होंने औद्योगिक विवाद निपटान के लिये जो नीति सुझाई उसे इतिहास में 'गिरी अप्रोच' कहा जाता है — यह समझौता एवं सामूहिक बातचीत पर जोर देता था और अनिवार्य निर्णय से पहले मध्यस्थता/समन्वय की शिफ़ारिश करता था। बाद में वे उत्तर प्रदेश, केरल तथा मैसूर/कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे।
उपराष्ट्रपति, अभिनय राष्ट्रपतित्व और 1969 का राष्ट्रपति चुनाव
13 मई 1967 को वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति ज़ाकिर हुसैन के 3 मई 1969 को निधन के बाद उपराष्ट्रपति गिरी को तत्काल कार्यवाहक राष्ट्रपति शपथ दिलाई गई। उस वर्ष का राष्ट्रपति चुनाव भारतीय राजनैतिक इतिहास में निर्णायक रहा — कांग्रेस पार्टी के अंदर “सिन्डिकेट” और प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के बीच मतभेद तेज़ हुए। गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर निर्वाचित राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और संकीर्ण अंतर से जीत गए — इस प्रक्रिया ने पार्टी के भीतर गहरे विभाजन को उजागर किया और केंद्र में राजनीतिक दिशा पर असर डाला।
राष्ट्रपति काल — प्रमुख निर्णय और नीतियाँ
राष्ट्रपति के रूप में और उससे भी पहले अभिनय राष्ट्रपति रहते हुए गिरी ने कुछ ऐतिहासिक और विवादास्पद निर्णयों पर अंतिम सहमति दी/आदेशित किए। जुलाई 1969 में, अभिनय राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधी अध्यादेश (Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance) पर अनुशासनिक सहमति दी — यह कदम बाद में 19 जुलाई 1969 के बैंक नेशनलाइज़ेशन के रूप में सामने आया और भारतीय अर्थव्यवस्था व राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा 1972 में हुए शिमला (Simla) समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के समय भी राष्ट्रपति पद की औपचारिक मंजूरी उनके कार्यकाल का हिस्सा रही। इन निर्णयों ने तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक नीतियों और भारत की बाहरी नीति दोनों पर असर डाला।
लेखन, सम्मान और पश्चात्कालीन जीवन
गिरी ने श्रम संबंधित विषयों पर कई लेख तथा संस्मरण लिखे — जैसे Industrial Relations and Labour Problems in Indian Industry और अपनी आत्मकथा My Life and Times (1976)। उनके सार्वजनिक जीवन के सम्मान स्वरूप 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 24 जून 1980 को उनका निधन हुआ; उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार दिया गया।
विरासत और मूल्यांकन
वराहगिरी वेंकट गिरी (V. V. Giri) की विरासत जटिल और बहुआयामी है — वे श्रमिक अधिकारों के अग्रदूत थे, जिन्होंने औद्योगिक संबंधों के मॉडल और श्रमिक आन्दोलन को औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया के साथ जोड़ा। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनके कुछ निर्णय (विशेषकर बैंक राष्ट्रीयकरण का समर्थन/आदेश) ने भारत के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को बदल दिया और साथ ही 1969 के चुनाव ने कांग्रेस पार्टी की आंतरिक राजनीति और देश के राजनीतिक विन्यास को प्रभावित किया। उनके नाम पर राष्ट्रीय श्रम संस्थान (V. V. Giri National Labour Institute) का नामकरण और 1974 में जारी डाक टिकट जैसे स्मारक उनके श्रमिक-प्रधान योगदानों की याद दिलाते हैं।
निष्कर्ष
वराहगिरी वेंकट गिरी (V. V. Giri) का जीवन श्रमिक संघर्ष, सार्वजनिक सेवा और संवैधानिक कर्तव्यों के बीच लगातार संतुलन खोजने का उदाहरण है। किसी समय वे जेल-यात्रा और हड़ताल के अधिवक्ता थे; बाद में उन्हीं अनुभवों के साथ वे राष्ट्र के उच्चतम संवैधानिक पद तक पहुँचे। उनके निर्णयों और नेतृत्व ने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और श्रम नीतियों पर स्पष्ट और दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ा — और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत मानी जाती है।













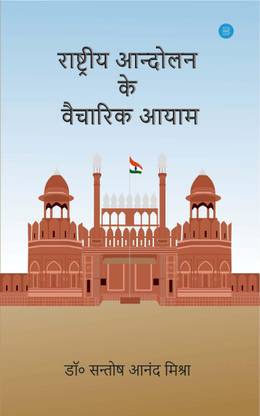





0 Comments
Thank you