भूमिका
डॉ. राममनोहर लोहिया (23 मार्च 1910 – 12 अक्टूबर 1967) भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के आकाश में एक तेजस्वी नक्षत्र हैं। वे मात्र राजनेता नहीं थे, बल्कि एक मौलिक दार्शनिक, इतिहासकार और अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने आजीवन सत्ता के बजाय सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। उनका समूचा जीवन सामाजिक न्याय, समानता और शोषण-मुक्त समाज की स्थापना के लिए समर्पित एक सतत संघर्ष था।
वैचारिक आधार: गांधी और समाजवाद का समन्वय
लोहिया के विचार गांधीवाद और समाजवाद का एक अनोखा मेल थे। जहाँ उन्होंने गांधीजी से सत्याग्रह, विकेन्द्रीकरण और नैतिक शुद्धता का पाठ सीखा, वहीं उन्होंने समाजवाद को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर प्रस्तुत किया। उनका समाजवाद पश्चिमी या मार्क्सवादी समाजवाद की नकल नहीं था, बल्कि यह भारतीय गाँवों, किसानों और जातिगत असमानताओं की समस्याओं पर केंद्रित था। वे मानते थे कि एशिया की समस्याओं का समाधान एशियाई तरीकों से ही होना चाहिए।
सप्त क्रांति: लोहिया का सामाजिक एजेंडा
लोहिया के विचारों का केंद्रीय स्तम्भ उनकी 'सप्त क्रांति' (सात क्रांतियाँ) का सिद्धांत था। यह सात क्रांतियाँ एक साथ लड़ी जाने वाली थीं ताकि समाज से हर प्रकार की असमानता और अन्याय को खत्म किया जा सके। ये सिर्फ नारे नहीं, बल्कि उनके समाज परिवर्तन के एजेंडे का मूल ढाँचा थे:
नर-नारी की समानता: स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर दिलाना।
रंगभेद का विरोध: चमड़ी के रंग पर आधारित राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता को समाप्त करना।
जाति प्रथा का विनाश: जन्मजात जाति प्रथा को तोड़ना और पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करना। उनका प्रसिद्ध नारा था: "पिछड़ा पावे सौ में साठ।"
विदेशी गुलामी के विरुद्ध: विदेशी दासता, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष।
आर्थिक समानता: निजी पूँजी की विषमताओं के विरुद्ध और आर्थिक समानता तथा योजना द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के लिए।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता: निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के ख़िलाफ़ और लोकतंत्री पद्धति के लिए।
हथियारों के विरुद्ध और सत्याग्रह के पक्ष में: अस्त्र-शस्त्र की होड़ का विरोध और अहिंसा व सत्याग्रह के मार्ग पर चलना।
लोहिया का मानना था कि इन सातों क्रांतियों को एक साथ चलाना होगा, क्योंकि ये सभी अन्याय आपस में जुड़े हुए हैं।
राजनीतिक दर्शन और 'गैर-कांग्रेसवाद'
स्वतंत्रता के बाद, लोहिया भारतीय राजनीति में एक प्रखर विपक्षी नेता के रूप में उभरे। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की नीतियों की तीखी आलोचना की। उनका 'गैर-कांग्रेसवाद' का सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं था, बल्कि यह सत्ता की जड़ता, भ्रष्टाचार और एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के खिलाफ एक वैचारिक संघर्ष था। उनका तर्क था कि लंबे समय तक एक ही पार्टी के शासन से लोकतंत्र कमजोर होता है।
उन्होंने छोटे दलों और पिछड़ों को एकजुट करने का नारा दिया ताकि एक मजबूत और सिद्धांतनिष्ठ विपक्ष का उदय हो सके।
भाषा और शिक्षा पर विचार
लोहिया ने भारतीय भाषाओं को, विशेषकर हिंदी को, सार्वजनिक और प्रशासनिक जीवन में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए 'अंग्रेजी हटाओ' आंदोलन चलाया। वे मानते थे कि अंग्रेजी केवल एक छोटे से अभिजात वर्ग को शासन करने की अनुमति देती है, जबकि आम जनता को विकास और न्याय से दूर रखती है।
इसके अलावा, उन्होंने 'चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान' का नारा देकर शिक्षा में समानता की वकालत की।
विरासत और प्रासंगिकता
डॉ. राममनोहर लोहिया का जीवन और विचार आज भी भारतीय राजनीति और समाज के लिए प्रकाशस्तंभ हैं। उनका सप्त क्रांति का सिद्धांत आज भी सामाजिक न्याय, आरक्षण, महिला सशक्तिकरण और रंगभेद के खिलाफ वैश्विक आंदोलनों में प्रासंगिक है। वे एक ऐसे सच्चे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि सड़क पर, गाँव में और आम आदमी के संघर्ष में अपनी जगह बनाई। वे न केवल समाजवादी आंदोलन के जनक थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को यह सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होती है।











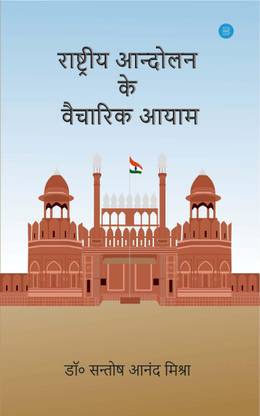





0 Comments
Thank you